भूकंपमापी (Seismometer) भूगति के एक घटक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से अधिक यथार्थतापूर्वक अभिलिखित करने वाला उपकरण है। सुपरिचित प्राकृतिक भूकंपों, भूमिगत परमाणु परीक्षण एवं पेट्रोलियम अन्वेषण आदि में मनुष्यकृत विस्फोटों तथा तेज हवा, समुद्री तरंग, तेज मानसून एवं समुद्री क्षेत्र में तूफान या अवनमन आदि से उत्पन्न सूक्ष्मकंपों (microseism)श् के कारण भूगति उत्पन्न हो सकती है। उचित रीति से अनुस्थापित (oriented), क्षैतिज भूकंपमापी भूगति के पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण के घटक को अभिलिखित करता है और ऊर्ध्वाधर भूकंपमापी ऊर्ध्वाधर गति,
चित्र १. ग्रे तथा यूईग का ऊर्ध्वाधर गति भूकंपमापी
अर्थात भूगति के ऊर्ध्वाधर घटक को अभिलिखित करता है। १९वीं शताब्दी के मध्यकाल के लगभग यांत्रिक भूकंपविज्ञान की नींव पड़ी, भूकंपमापियों का निर्माण हुआ और भूकंप अभिलेखन के लिये वेधशालाओं के जाल बिछ गए। इन दिनों रॉबर्ट मैलेट (Robert Mallet) द्वारा किया गया कार्य महत्वपूर्ण था। १८९२ ई० में जापान में जॉन मिल्न (Johan Milne) ने नॉट (Knott), यूईग (Ewing) और ग्रे (Gray) के सहयोग से सतह भूकंपमापी (compact seimometer) विकसित किया और तभी से विश्व के अनेक भागोें से यथार्थ यांत्रिक आँकड़े एकत्र करने में भूकंपमापियों का उपयोग होने लगा। भारत की कुछ प्रधान वेंधशालाओं (बंबई, कलकत्ता) में मिल्न भूकंपमापियों का उपयोग १८९८ ई० में प्रारंभ हुआ। १९०५ ई में शिमला, बंबई और कलकत्ते की वेधशालाओं में ओमोरी यूईग भूकंपमापी आ गए थे। इसके बाद अन्यान्य भूकंपमापियों का उपयोग अनेक वेधशालाओं में प्रारंभ हुआ।
यांत्रिक भूकंपमापी (जैसे मिल्न-शॉ भूकंपलेखी) में एक क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर लोलक होता है, जो उपलब्ध आधार शैल से सन्निहित पाए पर चढ़ा रहता है, या पृथ्वी में काफी गहराई में स्थित रहता है। काँपती पृथ्वी के कारण लोलक में उत्पन्न कंपनों को उपयुक्त युक्ति से प्रवर्धित और अभिलिखित किया जाता है। अवांछित दोलनों
चित्र २. मिल्न (Milne) का भूकंपमापी
अ ब = लोहे का स्तंभ, ब द = लोलक की बल्ली,
अ स = सहारा देनेवाला रेशम का डोरा, म = पीतल की दो गेंदों का लोलक तथा प = घूमने वाला बेलन, जिसपर ब्रोमाइड कागज चिपकाया है।
द पर एक रेखाछिद्र तथा उसके नीचे, खोखे के अंदर, समकोण दिशा में दूसरा रेखाछिद्र है। निकट के लैंप से प्राप्त तथा एक दर्पण से परावर्तित प्रकाश दोनों छिद्रों से गुजरकर, घूमते हुए ब्रोमाइड कागज पर गिरता है और इस प्रकार कंपनों के चित्र उसपर बन जाते हैं।
(oscillations) को निस्यंदित करने के लिये लोलक प्राय: क्रांतिक रूप से अवमंदित होता है। ऊर्ध्वाधर उपकरण के निम्नलिखित गणितीय विवेचन से भूकंपमापी का कार्यकारी सिद्धांत स्पष्ट हो जायगा।
मान लें कि किसी इमारत की धरन के स्थिर बिंदु से एक भारी संहति म (m), जो भारहीन कमानी से संबद्ध है, लटकाई जाती है। कमानी में निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में विस्थापन होगा:
(अ) निलंबित संहति पर अधोमुख बल के कार्य करने पर, तथा (ब) धरन में स्थिर बिंदु (निलंबन बिंदु) में किसी स्थिर अक्ष के संदर्भ में ऊर्ध्वमुख नियम गति (prescribed motion) होने पर।
इसलिये पृथ्वी की गति (यहाँ धरन की गति) चाहे जो हो, उसे यह मानकर निर्धारित किया जाता है कि निलंबित संहति पर एक बल कार्य करता है, जो संहति और धरन के ऋणात्मक त्वरण के गुणन के बराबर होता है। अत: गति का समीकरण यह होगा:
![]() श्
श्
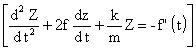
जहाँ वि (Z) = विस्थापन, क्रां (f) = क्रांतिक अवमंदन कारक, प्र (k) = कमानीका प्रत्यावर्तन बल निर्धारित करनेवाला प्रत्यास्थ स्थिरांक, सं (m) = संहति और त्व [f�] त्वरण तथा स (t)श् समय है। उपयुक्त स्थितियों में दो विभिन्न प्रकार के अभिलेख उपलब्ध होते हैं।
प्रथम स्थिति -- यदि प्रत्यावर्तन बल बहुत छोटा (k = o) और साथ ही अवमंदन अत्यल्प (f = o) हो तो समीकरण का निम्नलिखित रूप हो जाता है :
![]() श्
श्
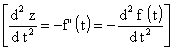
समीकरण (२) का इन परिसीमा प्रतिबंधों के साथ समाकलन करने पर कि आरंभ में स (t) = o, वि (z) = o और ता वि/ता स (dz/dt) = o हो तो हमें विश् (t)] = - त्व स [z = - f� (t)] प्राप्त होता है, अर्थात् संहति का वास्तविक गति पृथ्वीश् (धरण) की गति के ठीक विपरीत होती है। यह आदर्श भूकंपमापी है।
दूसरी स्थिति -- यदि पहले समीकरण में प्रत्यावर्तन बल अन्य कारकों की तुलना में बहुत बड़ा है, तो समीकरण घटकर
![]() श्
श्
हो जायगा। यहाँ विस्थापन वि (Z) पृथ्वी (धरन) के ऋणात्मक त्वरण का अनुपाती है। पृथ्वी के त्वरण का अभिलेखन करने के लिये यह भी एक आर्दश उपकरण है।
जैसा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, कुछ भूकंपलेखियों को भूकंपमापी के रूप में और कुछ को त्वरणमापी के रूप में अभिकल्पित किया जाता है। यांत्रिक भूकंपलेखियों में मिल्न शॉ और वुड ऐंडरसन उपकरण प्रधान हैं और भारत एवं विदेश की अनेक वेधशालाओं में काम में आते हैं।
मिल्न शॉ क्षैतिज घटक भूकंपमापी का उपकरणी विवरण - लोलक का आर्वतकाल स० (time period t0) १० से १२ सेकंड तक तथा अवमंदन अनुपात २० :१ होता है। आवर्धन प्रकाशिक सहित यांत्रिक है और स्थैतिक (static) आर्वधन १५० से २५० तक परिवर्तनीय है। लगभग ०.५ किलोग्राम भार की संहति ५० सेंमी० लंबे बल्ले (boon) से जोड़ दी जाती है। अवमंदन युक्ति के रूप में ताँबे की एक पट्टिका लोलक से जोड़ दी जाती है, जो चार नालचुंबकों के ध्रुवों के बीच गतिशील रहता है। चुंबकों की स्थिति का समंजन कर अवमंदन को समंजित किया जा सकता है।
वुड-ऐंडरसन (क्षैतिज) भूकंपमापी का उपकरण विवरण-- लगभग ०.७ ग्राम भार का ताँबे एक छोटा बेलन एक तने हुए उर्ध्वाधर तार पर उत्केंद्रत: चढ़ा होता है। तार कीश् मारोड़ी (torsiona) प्रतिक्रिया से नियंत्रण होता है। आर्वतकाल स० (t०) लगभग एक सेकंड होता है। शक्तिशाली चुबंक के ध्रुवों के बीच लटकती संहति के कारण क्रांतिक (critical) अवमंदन होता है। उपकरण का स्थैतिक आर्वधन प्राय: १,५०० से २,००० तक है।
विद्युच्चुबंकीय भूकंपमापी - विद्युच्चुबंकीय भूकंपलेखी, या भूकंप मापी में जड़त्वीय द्रव्यमान (inertial mass) चुबंक के ध्रुवों के मध्य गतिशाली रहता है। चालक तार की एक कुंडली संहति के चारों ओर लपेट दी जाती है, जिससे वह विद्युज्जनित्र (electric generator) की तरह काम करने लगती है। कुंडली में प्रेरित विद्युद्धारा जड़त्वीय द्रव्यमान और चुंबक के बीच की सापेक्ष गति, अर्थात् पृथ्वी के कंपन, पर निर्भर करती है। इस रीति से उत्पन्न विद्युद्धारा को उपयुक्त धारामापी द्वारा अभिलिखित कर लिया जाता है। बैनियॉफ उपकरण इस प्रकार के भूकंपमापी का अच्छा उदाहरण है। यह उपकरण क्षैतिज और ऊर्घ्वाधर दोनों प्रकार का होता है।
ये सभी उपकरण भूकंप या सूक्ष्मभूकंप को अभिलिखित करने के लिये अभिकल्पित होते हैं। इनके अलावा अनेक प्रकार के भूकंपमापी हैं, जो छोटे, सुवाह्य एवं प्राय: विद्युच्चुबकीय सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त अवमंदन आदि के साथ अभिकल्पित हैं और आजकल तेल आदि के भूकंपी पूर्वेक्षण में मनुष्यकृत विस्फोटनों से उत्पन्न अल्पकालिक तरंगो को अभिलिखित करने में काम आते हैं।
भूकंपमापियों के अभिलेखन - भूकंपमापियों का अभिकल्पन विभिन्न प्रकार की भूकंप तरंगों, प्रा (P), प्राथमिक, गौ (S), गौण तथा पृष्ठ तरंग आदि का अभिलेखन करने के लिये होता है, जो भूकंप के स्त्रोत से इस प्रकार प्रसर्जित (emanated) होती है कि कोई भी उनकी विभिन्न प्रावस्थाओं (phases) के अंतर को अभिलेख से जान सकता है। भूकंप के अधिकेंद्र की (epicentral) दूरी और फोकस की गहराई के अध्ययन के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रक्षण स्थल पर प्रा (P) और गौ (S) तरंगों के अभिलिखित अंतराल (interval) से प्रा (P) और गौ (S) तरंगो का वेग ज्ञात कर लिया जाता है, जिससे भूकंप के अघिकेंद्र की दूरी सीधे सीधे ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार स्थानीय भूकंपों के अभिलेख का अध्ययन पृथ्वी की पटलीय परतों और सुदूर होनेवाले भूकंपों से संबद्ध पृथ्वी के अंतराश की उपयोगी सूचनाएँ प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि भूकंपमापियों के अभिलेखों के आधार पर जो उन दिनों पर्याप्त सूक्ष्मग्राही न थे, ओल्डैम (Oldham) ने सुझाया कि पृथ्वी का क्रोड ठोस नहीं, संभवत: तरल है। आज जब भूकंपविज्ञान का विकास भूकंप इंजीनियरी और भूकंप सर्वेक्षण के रूप में हो चुका है, भूकंप और सूक्ष्मभूकंप के अध्ययन के अतिरिक्त भूकंपमापियों के महत्व की अत्युक्ति नहीं की जा सकती ।
[किरण चंद चक्रवर्ती]