बेतारी तारसंचार विद्युच्चुंबकीय तरंगों के उत्पादन एवं संप्रेषण संबंधी हर्ट्ज के प्रयोग (देखें, विद्युच्चुंबकीय तरंगें) के लगभग छह वर्षों के अनंतर, सन् १८९४ में, सर ऑलिवर लॉज नामक वैज्ञानिक ने बेतार के तार द्वारा संकेतप्रेषण का सर्वप्रथम सफल प्रयोग किया और सन् १८९७ ई. के लगभग प्रेषक एवं संग्राहक परिपथों के समस्वरण (tuning) का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सन् १८९४ में ही गूलिएल्मो मारकोनी (Gulielmo Marconi) नामक इंजीनियर ने बोलोन्या (Bologna) में बेतार के तार द्वारा वार्तावहन का सफल प्रदर्शन किया और १८९९ ई. में इंग्लिश चैनेल के उस पार बेतार का संकेत प्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। सन् १९०१ में मारकोनी ने न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन्ज़ नगर में एक पतंग से एरियल लटकाकर इंग्लैंड में कॉर्नवॉल के पोल्थू नामक स्थान से प्रेषित सिगनलों को ग्रहण किया।
मारकोनी द्वारा व्यवहृत व्यवस्था ऐतिहासिक एवं आधुनिक बेतार के तार की यांत्रिक प्रणाली के आद्य रूप में अप्रतिम महत्व की है। इसे नीचे चित्र १. में प्रदर्शित किया गया है। इसमें प्रत्येक बार कुंजी बंद करने पर रमकॉर्फ़ कुंडली (Rhumkorff's coil), या स्फुलिंग कुंडली, से उच्च विभव के स्पंदनों (pulses) की एक तरंगावलि (train) उत्पन्न होती है। प्रत्येक ऐसे स्पंदन (pulse) से प्लेट ग का विभव बढ़ता है और अंत में स्फुलिंग अंतराल (spark gap) च में स्फुलिंग विसर्जन होता है। प्लेट ग और पृथ्वी के बीच होनेवाला विसर्जन दोलनी (oscillatory) होता है और इसकी आवृत्ति दोनों के बीच स्थित ऊर्ध्वाधर तार की धारिता और प्रेरकत्व (inductance) पर निर्भर करती है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ आ (f) दोलन की आवृत्ति, ल (L) प्रेरकत्व तथा धा (C) धारिता है :
![]()
तार में इस प्रकार उत्पन्न दोलनी विद्युद्धारा से विद्युच्चुंबकीय ऊर्जा का विकिरण होता है। इससे दोलनी धारा की प्रबलता भी अत्यंत द्रुत गति से कम होती जाती है और प्लेट ग की वोल्टता भी अपना पुनरुत्थान होने तक अत्यंत
चित्र १.
क्षीणप्राय रह जाती है। इससे उत्पन्न तरंगों का रूप चित्र १. में नीचे प्रदर्शित है। चित्र २. में प्रदर्शित संयंत्र प्रणाली भी उपर्युक्त प्रणाली की ही भाँति कार्य करती है, किंतु इसमें प्रेषित्र एवं ग्राही के साथ एक एक समस्वरित परिपथ भी संबद्ध है। प्रेषित्र में संघनित्र ग प्रेरकत्व च और स्फुलिंग
चित्र २.
अंतराल घ भी सम्मिलित है। इसमें दोलनी धारा उत्पन्न होती है, किंतु मुख्य विकिरण सीधे इस परिपथ से नहीं, अपितु च और ग युक्त तथा आ (f) आवृत्ति के लिए अनुनाद करनेवाले समस्वरित परिपथ से होता है। इस प्रणाली के ग्राही तंत्र में एक संसूचक (detector) झ भी होता है, जो आपाती प्रत्यावर्ती धारा को सरल संकेत धारा में परिणित कर देता है। ज्ञातव्य है कि कुछ वर्षों के उपरांत फ्लेमिंग ने डायोड वाल्ब (diode valve) का आविष्कार किया, जिसने इस साधारण संसूचक का स्थान ले लिया, और उसके बाद ही ली डेफॉरेस्ट ने ट्रायोड वाल्ब (triode valve) का आविष्कार किया, जो दोलनी धारा उत्पादन के लिए रमकॉर्फ कुंडली एवं स्फुलिंग अंतराल के स्थान पर जनित्र के लिए प्रयुक्त होने लगा।
बेतार का तार प्रेषण - बेतार के तार द्वारा वार्तावहन, या संकेत संचार, की प्रक्रिया के तीन मुख्य अंग होते हैं : (१) बेतार के तार तरंगों (या रेडियो तरंगों) का उत्पादन एवं प्रेषण, (२) तरंगों का दिक् में गमन या संचरण और (३) रेडियो तरंगों का अभिग्रहण (reception)। तरंगों का उत्पादन एवं प्रेषण करनेवाली यंत्र प्रणाली को बेतार प्रेषित्र (wireless transmitter) कहते हैं। संचरणेपरांत ये तरंगें एक ग्राही (receiver) में संगृहीत होती हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। इसका सामान्य विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।
बेतार तरंगों का उत्पादन एवं प्रेषण - बेतार का तार प्रेषित्र विद्युत् की अत्यंत द्रुत, दोलनी गति उत्पन्न करनेवाली एक यंत्रव्यवस्था होती है, जिससे दिक् में विद्युत्तरंगों की उत्पत्ति होती है। इस व्यवस्था के तीन मुख्य भाग होते हैं: (१) उच्च आवृत्ति के दोलन उत्पन्न करनेवाला एक जनित्र (generator), (२) दोलनों का कुंजीयन (keying) अथवा अधिमिश्रण (modulation) करने का एक साधन, तथा (३) इस प्रकार उत्पन्न दोलनों को अभीष्ट शक्तिस्तर तक प्रवर्धित करने का उपयुक्त साधन। जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, प्रारंभ में स्फुलिंग प्रेषित्र (spark transmitter) का प्रयोग किया जाता था, किंतु १९४१ ई. में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध द्वारा स्फुलिंग प्रेषित्रों का प्रयोग निषिद्ध मान लिया गया। उनका स्थान बाल्व संयंत्रित एवं क्रिस्टल संयत्रित दोलकों ने ले लिया। कहीं कहीं आर्क संयंत्रित दोलकों का भी प्रयोग अभी तक किया जा रहा है।
हर्ट्ज़ द्वारा प्राप्त परिमाणों का विस्तृत गणितीय विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि एक ऐसे वैद्युत द्विक् (electric doublet) से, जिसके वैद्युत आघूर्ण (electric moment) में आवर्ती परिवर्तन होता रहता है, र (r) दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर विद्युच्चालक तक पहुँचनेवाला विद्युद्बल निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात होता है :
![]() . . . . . . . . . . . (१)
. . . . . . . . . . . (१)
यहाँ हस (hs) = चालक की लंबाई, घस (is) = चालक में प्रवाहित होनेवाली प्रत्यावर्ती धारा का आयाम (amplitude) तथा त (l)=धारा की कोणीय आवृत्ति है। समीकरण (१) में घस (is), हस (hs), र (r) और त (l) मीटरों में व्यक्त किए गए हैं और व (E) वोल्ट प्रति मीटर में व्यक्त किया गया है। इसे व्यावहारिक प्रेषणसूत्र कहते हैं। प्रेषित्र में उपर्युक्त चालक को एरियल (aerial) कहा जाता है। सूत्र (१) से स्पष्ट है कि एरियल का ऊँचाई (hs) हस, जितनी ही अधिक होगी, और आवृत्ति, १/त (१/l) जितनी ही अधिक होगी, उतना ही अधिक विद्युद्बल उस एरियल में कार्यशील होगा। ऐसा स्थिर विद्युद्वाही उर्ध्वाधर एरियल वस्तुत: एक उर्ध्वाधर तार मात्र होता है, जिसका शीर्ष लंबा एवं चौरस होता है (चित्र ३.)। ऑलिवर लॉज द्वारा प्रवर्तित विधानुसार इसमें एक प्रेरकत्व ल (L) का भी समावेश कर लिया जाता है जिसके कारण यह व्यवस्था दोलनकारी हो जाती है। इससे उस परिपथ में अवमंदित विद्युद्दोलकों के ्ह्रास की दर में कमी होने के अतिरिक्त परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के समंजन के एक सुगम उपाय का भी समावेश हो जाता है। प्रेषण के लिए दीर्घकालिक दोलन उत्पन्न करनेवाले एक तापायनिक (thermionic) वाल्व द्वारा इसे ऊर्जित करते हैं। एरियल में अधिकतम धारा उत्पन्न करने के लिए परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति, दोलन
चित्र ३.
उत्पन्न करनेवाले उपर्युक्त वाल्व के दोलन की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। व्यवहार में एरियल के समग्र उर्ध्वाधर भाग अ ब में विद्युद्धारा प्राय: स्थिर रहती है, किंतु क्षैतिज भाग ब स में धारा की प्रबलता तथा पृथ्वी के सापेक्ष विभव का मान लंबाई की ओर बदलता जाता है। इसके अतिरिक्त, इस अंश का प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध इसकी संपूर्ण लंबाई में वितरित रहते हैं और इस संपूर्ण भाग के लिए इनके मान दोलन की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। बेतार प्रेषित्रश् के लिए उपयुक्त एरियल का चयन करते समय उसके प्रतिरोध, प्रेरकत्व एवं धारिता के लिए उसकी स्वाभाविक आवृत्ति एव उससे उत्पन्न तरंगदैर्ध्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। गणितीय विश्लेषण से इनके लिए निम्नलिखित व्यंजक प्राप्त होते हैं:
स्वाभाविक आवृत्ति, आ =
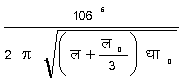
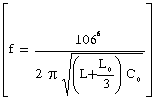
एवं तरंग लंबाई, त
= 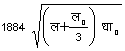
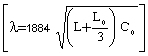
जहाँ ल (L) ऊर्ध्वाधर भाग में निहित प्रेरकत्व है, ल० (L0) तथा धा० (C0) क्षैतिज भाग ब स के क्रमश: प्रेरकत्व एवं धारिता हैं। एरियल परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध वस्तुत: चार प्रतिरोधों का योग होता है, जो क्रमश: क्षैतिज भाग का प्रतिरोध, कुंडली प का प्रतिरोध, विकिरण प्रतिरोध एवं उर्ध्वाधर भाग का प्रतिरोध है। विकिरण प्रतिरोध, तरंगों के रूप में ऊर्जा के विकिरण के कारण प्रतिरोध में होनेवाली वृद्धि है, जो परिमाण में उस प्रतिरोध के बराबर होती है जिसे ऊर्ध्वाधर भाग में रखने पर, उसके द्वारा उतनी ही ऊर्जा का अवशोषण होता जितनी ऊर्जा तरंग के रूप में विकिरित होती है। उपर्युक्त दृष्टांत में प्रदर्शित चौरस शीर्ष एरियल के लिए विकिरण प्रतिरोध का मान निम्नलिखित होता है :
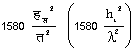 ओम।
ओम।
बेतार तरंगों का संग्रहण - उपर्युक्त प्रेषित्र प्रणाली द्वारा उत्सर्जित विद्युत्तरंगों के कारण र (r) दूरी पर स्थित, हर (hr) ऊँचाई के संग्राही एरियल के किसी बिंदु पर ब.हर (E hr) वोल्ट का विद्युद्वाहक बल (electromotive force) उत्पन्न होता है। यहाँ ब (E) उस प्रेषित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत् क्षेत्र की तीव्रता है जो सूत्र (१) द्वारा व्यक्त होता है। इस संग्राही एरियल को एक प्रेरकत्व की सहायता से आगत विद्युत् की आवृत्ति के लिए समस्वरित किया जा सकता है। अनुनाद की दशा में संगृहीत संकेतधारा संग्राही एरियल में विद्युद्धारा के रूप में नहीं, अपितु इसी प्रेरकत्व के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युद्वाहक बल के रूप में, संसूचित (detect) हो सकती है। इसे एक विभव प्रवर्धक (potential amplifier), यथा तापायनिक वाल्व प्रवर्धक, द्वारा प्रवर्धित कर क्रिस्टलीय या वाल्व संसूचक में प्रविष्ट किया जाता है। इस प्रकार यह उस क्रिस्टल परिपथ या वाल्व के धनाग्र परिपथ में सरल धारा में रूपांतरित हो जाता है और टेलीफोन या धारामापी (galvanometer) की सहायता से अपना अस्तित्वबोध कराता है।
दिशात्मक एरियल (Directive Aerial) - उपर्युक्त व्यवस्था में किंचित् सुधार कर उसे दिशात्मक एरियल में भी परिणत किया जा सकता है। यदि खुले तार के स्थान पर एक बंद कुंडली या पाशकुंडली (loop) का प्रयोग एरियल के रूप में किया जाए (चित्र ४, अ ब द स), तो दोनों ऊर्ध्वाधर भुजाओं में उत्पन्न विद्युत्द्वाहक बलों की कलाओं में अंतर होने के कारण एक परिणामी विद्युत्बल, बर (Er), उस कुंडली में कार्य करने लगेगा, जिसका परिमाण निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रकट होता है :
![]()
यहाँ अ (A) कुंडली का क्षेत्रफल तथा न (N) उसमें तार के चक्करों की संख्या है। अनुनाद (resonance) की दशा में इससे एक दोलनी
चित्र ४.
धारा धर (ir) उत्पन्न हो जाती है, जिसका मान निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त होता है :
![]()
जहाँ प (R)
उस कुंडली का प्रभावकारी प्रतिरोध है। ऐसे ऐरियल को एक
संघनित्र, स (C) की सहायता से समस्वरित किया
जाता है, जिसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न दोलनी विभव
के रूप में संकेत पुनरुत्पादित होता है। इस विभव का आयाम
![]() श्के
बराबर होता है। इस एरियल के अक्ष की लंबवत् दिशा आनेवाली
तरंगों से इसमें अधिकतम संकेत तीव्रता उत्पन्न होती है और
अक्ष की ही दिशा में आनेवाली तरंगों से शून्य या न्यूनतम संकेततीव्रता
उत्पन्न होती है।
श्के
बराबर होता है। इस एरियल के अक्ष की लंबवत् दिशा आनेवाली
तरंगों से इसमें अधिकतम संकेत तीव्रता उत्पन्न होती है और
अक्ष की ही दिशा में आनेवाली तरंगों से शून्य या न्यूनतम संकेततीव्रता
उत्पन्न होती है।
बेतार के तार मोर्स संकेत (Morse signal) भेजने के लिए प्राय: दो विधियों का व्यवहार किया जाता है: एक में तो विराम के लिए शून्य आयाम (amplitude) के तथा डॉट (dot) एवं डैश (dash) के लिए नियत आयामों के संकेत प्रेषित किए जाते हैं। शून्य आयाम के संकेत को अंतरण अंतराल (spacing interval) तथा डॉट और डैश के संकेतों को चिह्नन अंतराल (marking interval) कहते हैं। दूसरी विधि में अंतरणी अंतरालों में चिह्न अवधि की अपेक्षा भिन्न तरंग लंबाई की तरंगें प्रेषित की जाती हैं, किंतु ग्राही को ऐसा समस्वरित किया जाता है कि वह चिह्नन अंतराल की ही तरंगों को ग्रहण कर सके।
तरंगों का संचरण या दिग्भ्रमण - बेतार के तार की तरंगों के दिक् में संचरण की प्रक्रिया का अध्ययन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना पड़ता है :
१.����� दीर्घ तरंगों के संचरण पर विचार करते समय निम्नलिखित बातें विशेष रूप से विचारणीय होती हैं : (अ) लघु दूरियों तक संचरण, जिनके लिए पृथ्वी को प्राय: समतल माना जा सकता है तथा (ब) दीर्घ दूरियों तक संचरण, जिनके लिए पृथ्वी की वक्रता को भी ध्यान में रखना पड़ता है।
२.����� लघु तरंगों का संचरण - इन तरंगों की लंबाई २०० मीटर से कम होती है और इनके संचरण की प्रक्रिया और दिशाएँ दीर्घ तरंगों के संचरण से सर्वथा भिन्न होती है।
३.����� तरंगसंचरण के लिए रात और दिन की दशाएँ बहुधा भिन्न होती है। लघु तरंगों के संचरण में इन दिशाओं का प्रभाव उल्लेखनीय होता है।
लघु दूरी तक बेतार का तार प्रेषण - बेतार के संकेतों को थोड़ी दूर तक प्रेषित करने में सागरपार और स्थलपार दशाओं में अंतर होता है। सागरपार प्रेषण में प्रेषित संकेतधारा तथा दूरी का गुणनफल दूरी बढ़ने के साथ घटता है। रात्रि में यह परिवर्तन अधिक अनियमित हो जाता है और दूरी बढ़ने के साथ साथ अनियमितता भी बढ़ती जाती है। लगभग १०० से १५० मील की दूरी पर प्राप्त संकेतों की तीव्रता रात्रि में शून्य से लेकर दिवसीय मान की दूनी तक हो सकती है। अधिक दूरियों पर रात्रि के समय संकेतों की तीव्रता दिन की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाती है।
रेडियो संकेतों में यह परिवर्तन समझने के लिए यह जान लेना अवश्यक है कि प्रेषित्र से ग्राही तक रेडियो तरंगें वायुमंडल के आयनोस्फ़ियर क्षेत्र के केनेली हेवीसाइड स्तर (Kennely heaviside layer) से परावर्तित होकर पहुँचती हैं (चित्र ५.)। जैसा चित्र से प्रदर्शित है, प्रेषित्र से तरंगे आयनोस्फ़ियर की ओर जाती हैं। इन्हें वायुमंडलीय किरण कहते हैं। दूसरी किरण धरती के समांतर ही जाती है। इसे भूमिकिरण कहते हैं। जब वायुमंडलीय किरण आयनोस्फ़ियर से परावर्तित होकर ग्राही पर उसी कला में पहुँचती है जिसमें भूमिकिरण पहुँचती है, तब संकेत की तीव्रता अधिकतम
चित्र ५.
होती है। दिन के समय आयनोस्फीयर का निम्नतम स्तर काफी नीचे तक आ जाता है और रात्रि में यह ऊपर चला जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि आयनोस्फ़ियर में वायु के आयनीकरण की क्रिया सूर्य की किरणों से प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न तरंगदैर्घ्यों का परावर्तन आयनोस्फ़ियर की विभिन्न सतहों से होता है। सामान्यत: अधिक लंबी तरंगों का परावर्तन उसकी निचली सतहों से और लघु तरंगों का परावर्तन ऊपर की सतहों से होता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अधिक दूरी तक रेडियो संकेतों के प्रेषण के लिए लघु तरंगों का उपयोग ही समीचीन होता है, क्योंकि ये ऊपरी सतहों से परावर्तित होने के कारण बहुत दूर तक, ऊर्जा का अधिक ्ह्रास हुए बिना ही, पहुँच सकती हैं। यह तथ्य चित्र ५. से स्पष्ट हो जाता है।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विभिन्न दूरियों पर रेडियों संकेतों की धूमिलता का स्पष्टीकरण किया जा सकता है।
कम दूरियों (यथा ५० मील) पर भूमिकिरण सीधे ग्राही तक पहुँच जाती है, जिससे रेडियों संकेतों की तीव्रता प्राय: अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि इसकी तीव्रता दिन और रात के समय समान रहती है। अधिक दूरियों (यथा १०० से १५० मील) पर, रात्रि में अपरिवर्ती भूमि किरण के साथ साथ प्राय: उसी तीव्रता की वायुमंडलीय किरणें भी ग्राही तक पहुँचती हैं। चूंकि ये अधोगामी तरंगें तीव्रता और कला, दोनों में ही, भूमिकिरणों से भिन्न होती हैं, इसलिए भूमिकरणों के साथ इनके संयोजन से उत्पन्न परिणामी संकेतों की तीव्रता शून्य से लेकर अहर्मान (daytime value) की दूनी तक हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों किरणें विपरीत या समान कलाओं में संयोजित होती हैं। और भी अधिक दूरियों पर भूमि किरणों की तीव्रता बहुत घट जाती है। इस कारण प्राप्त होनेवाले संकेत पूर्णतया अधोगामी (परावर्तित) वायुमंडलीय किरणों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। फलस्वरूप इनकी तीव्रता में परिवर्तन तो पर्याप्त सीमा तक हो सकता है, किंतु संकेत पूर्णतया लुप्त नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न तरंग लंबाइयों के लिए वह दूरी, जिसपर समान तीव्रतावाली वयुमंडलीय एवं भूमिकिरणें पहुँच सकती हैं, भिन्न भिन्न होती है। लगभग १,६०० मीटर तरंगदैर्ध्य वली तरंगों के लिए यह दूरी रात्रि में प्राय: ४८० से ६४० किलोमीटर तक होती है, पर १०० मीटरवाली तरंगों के लिए यह दूरी केवल १६० किलोमीटर के ही लगभग होती है।
दिशात्मक एरियलों (directive aerials) के द्वारा प्राप्त होनेवाले संकेतों में भी रात्रि और दिन का अंतर स्पष्ट परिलक्षित होता है। जैसा पहले बतलाया जा चुका है, ऐसे ऐरियलों को घुमाकर ऐसी स्थिति में लाया जाता है कि उनके द्वारा गृहीत संकेतों की तीव्रता अधिकतम हो। उस दशा में इस एरियल का अक्ष आगत तरंगों की दिशा के लंबवत् होता है। दिन में तो यह ठीक परिणाम देता है, किंतु रात्रि में ९० अंश तक की त्रुटि हो जाती है।
दीर्घ-दूरी रेडियो-तरंग-प्रेषण - ऊपर बतलाया जा चुका है कि मारकोनी ने सन् १९०१ में ही ऐटलैंटिक महासागर के पार तक बेतार के तार का संकेत भेजने में सफलता प्राप्त की थी, किंतु इसका स्पष्टीकरण हर्ट्ज़ के विवेचन के आधार पर प्राप्त प्रेषणसूत्र (१) द्वारा नहीं हो सका। इसलिए उपयुक्त सूत्र की प्राप्ति के प्रयत्न होते रहे। सन् १९१० में ऑस्टिन ने दीर्घ दूरी तक रेडियो-तरंग-प्रेषण का सुविस्तृत अध्ययन किया और र (r) दूरी पर किसी एरियल पर उत्पन्न विद्युत्बल के लिए निम्नलिखित संशोधित सूत्र प्राप्त किया :
ब=
![]() .e
- (०.००१५
र/�त)
.e
- (०.००१५
र/�त)
![]()
जहाँ घातांकीय पद (exponential term) को अवशोषण पद (absorption term) कहा जाता है। यह सूत्र केवल दिन के समय तरंगप्रेषण के लिए व्यवहृत होता है तथा केवल लगभग ४०० किमी. के लिए ही सत्य सिद्ध होता है। फुलर (Fuller) ने इस सूत्र में उपयुक्त संशोधन करने की चेष्टा की और अंत में अधिक दूरी तक अधिक लंबाई की तरंगों के लिए अहर्निश व्यवहार्य, व्यापक सूत्र
![]()
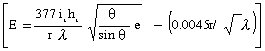
का प्रतिपादन किया, जिसमें q प्रेषक एवं अभिग्राही केंद्रों के बीच भू-केंद्रिक कोण (geocentric angle), अर्थात् पृथ्वी के केंद्र से दोनों स्थानों को मिलानेवाली रेखाओं के बीच बननेवाला कोण, है।
हर्ट्ज के प्रारंभिक प्रयोगों से यह अनुमान किया जाता था कि दीर्घ लंबाई की तरंगें अधिक दूर तक बतार वार्तावहन के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, किंतु तापायनिक वाल्वों का आविष्कार होने पर लघुतरंगों के साथ प्रयोग किए गए, जिनसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए : (१) लघु तरंगें बहुत अधिक दूरी तक, बिना अधिक ऊर्जाक्षीणन (attenuation) हुए ही, संचरित हो सकती हैं। इस कारण ऐसी तरंगों में अभीष्ट संकेतों के सफल संचरण के लिए निम्नशक्ति के प्रेषी केंद्रों (low power transmitting stations) की स्थापना की ही आवश्यकता पड़ती है; (२) यद्यपि लघु तरंगों के संकेतों की तीव्रता अल्प दूरी तक दूरी में वृद्धि के साथ घटती है, किंतु एक निश्चित दूरी तक दूरी में वृद्धि के साथ घटती है, किंतु एक निश्चित दूरी पार करने के पश्चात् इन संकेतों की तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। इस विशिष्ट, या निश्चित, दूरी को मूकांतराल (Skip distance) कहते हैं। यह दूरी सामान्यतया तरंग लंबाई, त (l) के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए लघु तरंगों के लिए इनका मान काफी अधिक होता है; (३) लघु तरंगों के लिए ऐसी अनुकूलतम (optimum) दूरियों के दो मान होते हैं : एक दिन के समय तरंगसंचरण के लिए और दूसरा रात्रि के समय के लिए। इसलिए इनके सम्मिलित प्रयोग से वार्तावहन का क्रम अहर्निश कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता है।
विकिरणों को अधिक प्रभावी एवं शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें एक पुंज के रूप में संघनित करने के उद्देश्य से, सर्वप्रथम मारकोनी कंपनी के इंजीनियरों ने तथा उनके पश्चात् फ्रैंकलिन ने, नए प्रकार के एरियल के निर्माण किए। इन एरियलों में समांतर ऊर्ध्वाधर तारों का एक फ्रेम प्रयुक्त किया गया था और उसके पीछे ठीक ऐसा ही एक अन्य फ्रेम भी रखा जाता था। इस पृष्ठस्थ फ्रेम को परावर्तक पर्दा (Reflecting Screen) कहा जाता था। इस व्यवस्था के दो लाभ हैं : (१) पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र से विद्युत्तरंगशक्ति का एकत्रीकरण, जिससे अपाती संकेतों की तीव्रता बढ़ जाती है, और (२) अन्य अवांछनीय संकेतों का परावर्तक द्वारा निस्यंदीकरण, जिससे वांछित संकेत अन्य संकेतों द्वारा व्यतिकृत न हो सकें।
सौर प्रभाव (Solar Influence) - ऑस्टिन ने सर्वप्रथम पता लगाया था कि सौर सक्रियता से भी बेतार की तरंगें प्रभावित होती हैं। जिन दिनों सूर्य के धब्बे (Sunspots) अधिक दिखलाई पड़ते हैं, उन दिनों रेडियों संकेतों की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। चुंबकीय तूफानों के दिनों में भी संकेतों की तीव्रता अन्य दिनों की अपेक्षा भिन्न हो जाती है। देखा गया है कि ऐसे दिनों में लघु तरंग संकेत निर्बल एवं दीर्घ तरंगसंकेत प्रबल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि सौर सक्रियता के कारण वायुमंडल के आयनोस्फ़ियर में आयनीकरण का परिमाण बढ़ जाता है। इस कारण उसमें होकर ऊपर तक जाने और वहाँ से परावर्तित होकर (और यह परावर्तन भी पूर्ण परावर्तन की ही भाँति वायुमंडलीय किरणों के विरल माध्यम में प्रवेश करने पर मुड़ने की क्रमिक क्रिया द्वारा होता है) आनेवाली तरंगों का बहुत कुछ अवशोषण वायुमंडलीय परतों में हो जाता है। इसलिए दीर्घ तरंगें तो, वायुमंडल के निम्नतम स्तरों से परावर्तित होने के कारण, प्राय: अप्रभावित रहती हैं, किंतु लघु तरंगों का काफी अंश अवशोषित हो जाता है। ऑस्टिन ने '११ वर्षीय चक्र' (11 year cycle) के अनुसार भी रेडियो संकेतों की तीव्रता में परिवर्तन का अध्ययन किया और यह पता लगाया कि दीर्घ तरंगों का परावर्तन करनेवाले वायुमंडलीय स्तर की विशिष्ट विद्युच्चालकता अधिकतम सूर्यकलंक के दिनों में न्यूनतम कलंकों के दिनों की अपेक्षा १.५ गुना अधिक होती है।
बार्तावहन के लिए बेतार के तार का प्रयोग - यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वार्तावहन के लिए उपयोगिता की दृष्टि से बेतार के तार का महत्व अप्रतिम है। दूरस्थ केंद्रों के बीच, विशेषकर समुद्रपार वार्तावहन के लिए, यह सागरगर्भी तार के केबुलों की अपेक्षा अधिक सुगम, सस्ता एवं उपयोगी साधन है। इसके लिए प्रेषित्र एवं अभिग्राही केंद्रों का निर्माण अपेक्षाकृत कम व्ययसाध्य है, क्योंकि सागरगर्भी केबुलों को दीर्घ दूरियों तक बिछाने में अत्यधिक धनराशि व्यय होती है। इसे अतिरिक्त एक और सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि रेडियों तरंग प्रेषित्र से चतुर्दिक् समान रूप से विकीर्ण होती है। इसलिए आवश्यक ग्राही उपकरण की व्यवस्था होने पर इस विधि से प्रेषित सूचना, समाचार अथवा वक्तव्य संसार के भिन्न भिन्न भागों में एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। संकटग्रस्त जहाजों से बेतार के तार द्वारा अपनी रक्षा के लिए की गई गुहार इस प्रकार चारों ओर बिखरती है और उनके समीपस्थ जहाज तथा अन्य यान उनकी सहायता के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त बेतार के तार द्वारा दूर से चित्र, फोटोग्राफ, पत्रादि, लेखों की प्रतिलिपियाँ अति शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित की जाती हैं।
एक कठिनाई, जिसका सामना सागरगर्भी केबिलों के उपयोग में करना पड़ता है, यह है कि यदि उनमें कहीं क्षरण (leakage) होता है, या वे कहीं टूट जाते हैं, तो उनका पता लगाना अथवा मरम्मत कर सकना बड़ा कठिन एवं अधिक समय में संपन्न होनेवाला कार्य होता है। इसके लिए टूटे हुए केबिल के पार्श्व में एक अन्य केबिल बिछाकर उसे वार्तावहन के लिए प्रयुक्त करने और उसके बाद ही क्षतिग्रस्त केबिल की मरम्मत करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी कठिनाई का हल करने के लिए अब प्रत्येक केबिल का प्रतिरूप (duplicate) भी साथ ही बिछाया जाता है, किंतु बेतार के प्रेषित्र या ग्राही सेट के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत करने में, या उसके स्थान पर दूसरे सेट की स्थापना में, कोई ऐसी कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती।
बेतार के तार से समाचार या संवादप्रेषण में भी एक बड़ी कठिनाई यह होती है कि प्रेषित संवाद की गोपनीयता की रक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा संवाद कहीं भी और किसी भी उपयुक्त ग्राही द्वारा सुना जा सकता है। इसलिए बड़े बड़े समाचार अभिकरणों अथवा समाचारपत्रों के प्रतिनिधि अपने समाचारों को बेतार के तार से न भेजकर साधारण तार द्वारा ही भेजना ठीक समझते हैं, अन्यथा वे समाचार उनके अभिकरण या पत्र द्वारा ही पहले न प्रकाशित होकर उसे ग्रहण करनेवाले अन्य अभिकरणों या पत्रों द्वारा लगभग उसी समय प्रकाशित हो सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय समझौता - चूँकि बेतार के तार के प्रेषित्र एवं ग्राही केंद्र विश्व भर में फैले हुए हैं, इसलिए यह संभव है कि विभिन्न केंद्रों से एक समय में एक ही तरंगदैर्ध्य, अथवा आवृत्ति, का प्रेषण होने पर वे ग्राही केंद्रों पर एक दूसरे को आवृत्त या व्यतिकृत कर लें। इससे बड़ी कठिनाइयाँ एवं समस्यएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए १९०६ ई. में बर्लिन के तथा १९१२ ई. में लंदन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रत्येक देश के बेतार के तार केंद्रों तथा जहाजों आदि से प्रेषित होनेवाली तरंगों की लंबाइयाँ निश्चित कर दी गई हैं तथा इसकी मान्यता के लिए संसार के प्राय: सभी प्रमुख देशों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर कराया गया। विभिन्न सेवाओं एवं प्रयोजनों के लिए, दीर्घ एवं लघु तरंगों द्वारा प्रेषणीय संकेतों की आवृत्तियाँ एवं तरंग लंबाइयाँ निश्चित कर दी गई हैं।
सागरीय यानों में भी बेतार के तार का व्यापक उपयोग होता है। सन् १९१४ के 'मेरी कन्वेन्शन' में यह निश्चय किया गया कि ऐसे सभी जलयानों में, जिनमें ५० या इससे अधिक यात्रियों का वहन होता हो, बेतार के तार के प्रेषित्र एवं ग्राही यंत्रों की स्थापना अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक यान में बेतार के तार की एक अतिरिक्त संचारी व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिसका प्रयोग मुख्य व्यवस्था के निष्क्रिय होने, या क्षतिग्रस्त होने, पर किया जा सके। आधुनिक जलयानों में बेतार के तार के स्थान पर अब रेडियों टेलीफोन का उपयोग बढ़ रहा है।
दिशाबोध (Direction Finding) - युद्धकाल की आवश्यकता से प्रेरित होकर, प्राय: सभी बड़े देशों के बंदरगाहों एवं उड्डयन केंद्रों पर दिशानिर्देशक एवं दिशान्वेषी संयत्रों की भी स्थापना की गई है। इनमें शक्तिशाली प्रेषित्र एवं ग्राही के अतिरिक्त दिशात्मक एरियल भी होते हैं। ये ऐरियल घूर्णनशील होते हैं। बंदरगाह या हवाई अड्डे से अपनी ओर आनेवाले यानों के साथ बेतार के तार के संकेतों का आदान प्रदान होता है और इन स्थानों पर स्थित एरियल को घुमा कर उनके अक्ष को ऐसी दिशा में लाया जाता है कि यान से आनेवाले संकेत तीव्रतम प्राप्त हों। इससे यान की गमन की दिशा बंदरगाह या अड्डे के किस ओर है, ज्ञात हो जाता है। कुहरे या धुंध से ढके वातावरण में इन यानों को इस विधि से यथावश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया जा सकता है। बहुधा ऐसा भी होता है कि ऐसे एरियल यान में ही होते हैं और बंदरगाह या हवाई अड्डे से आनेवाले संकेतों की सहायता से वे स्वयं अपनी उचित दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। कुछ विशेष प्रकार के घूर्णनशील एरियल भूमि पर स्थित, एक निश्चित केंद्र पर कुछ विशेष प्रकार के मोर्स संकेत प्रेषित करते हुए निरंतर घूर्णन करते रहते हैं और कुछ मानक स्थितियों में वे विशेष संकेत प्रेषित करते हैं। यानों में स्थित ग्राही उन संकेतों को ग्रहण करते हैं और उनकी सहायता से अपनी स्थिति का ज्ञान करते हैं। इन एरियलों का व्यापक उपयोग द्वितीय विश्वयुद्ध में आविष्कृत रेडार तंत्र में किया गया था। फ्रांस के तट से ध्वनिहीन 'वी' जेट वायुयानों के इंग्लैंड की ओर निरंतर प्रहारात्मक उड़ानों से इंग्लैंड आतंकित हो गया था। दिन में तो इन्हें देख सकना किसी प्रकार संभव भी था, किंतु रात्रि के समय, अथवा कुहरे या धुंध से आच्छादित आकाश में, इनकी गतिविधि पर दृष्टि रखना संभव नहीं था। ऐसे समय में इंग्लैड के तट से इन्हीं एरियलों द्वारा बेतार के तार के सकेत चतुर्दिक् प्रेषित किए जाते थे और इन्हीं एरियलों के निकट ग्राही यंत्र भी स्थापित किए गए थे। यदि शत्रु का कोई विमान तट की ओर आता था, तो इन संकेतों का द्रुत गति से परावर्तन होता था, जिसे ग्राही यंत्र व्यक्त करता था। उस विमान की गति, दिशा, स्थिति आदि इस प्रकार ज्ञात करके उसे प्रहार का लक्ष्य बनाया जा सकता था। (सुरेशचंद्र गौड़)