द्विखुरीयगण
(आर्टियोडैक्टाइला,
Artiodactyla)
गाय, भैंस, सूअर,
बकरी, ऊँट, हरिण
आदि स्तनियों
(mammals) का
गण है, जिनमें
गर्भनाल (placents),
पैर की सम अँगुलियाँ
तथा खुर होते
हैं। इस गण में खरगोश
से लेकर भैंस
और हिप्पोपोटैमस
जैसे भिन्न भिन्न
आकार प्रकार
के प्राणी सम्मिलित
हैं।
प्रधान
विशेषताएँ - प्रत्येक
पैर में शल्कीभूत
(cornified)
खुर से घिरी
हुई दो क्रियाशील
पादांगुलियाँ
होती हैं, पैरों
के अक्ष पादांगुलियों
के मध्य में होते
हैं। बहुतों के
सिर पर सींग
या शृंगाभ (antlers)
होते हैं। सूअर
को छोड़कर सब
का दंतविन्यास
हीन कोटि का
होता है। इनका
आमाशय चार
कक्षों में बँटा
होता है ओर
ये जुगाली करते
हैं। कुछ पाले जाते
हैं और कुछ का
शिकार किया
जाता है। आस्ट्रेलिया
को छोड़कर ये
सभी महाद्वीपों
में पाए जाते हैं।
इस गण के कुछ महत्वपूर्ण
परिवारों का
वर्णन निम्नलिखित
है :
 सुइडी
(Suidae)
- इनका
थूथन लंबा एवं
शंक्वाकार होता
है, जिनके चकतीनुमा
ऊर्ध्वाधर सिरे
पर चीरे से
नासारध्रं होते
हैं। इनका सिर
लंबा होता है,
आँख, कान छोटे
होते हैं और
मुँह मांसभक्षियों
की तरह चीरा
(cleft) होता
है। इनमें दाँतों
का पुरा समूह
(set) होता
है, काटनेवाले
निचले दाँत बाहर
की ओर उभरे
होते हैं और
नर के बड़े बड़े भेदक
दाँत (canines)
हाथी के दाँत
के समान मुँह
के बाहर निकले
होते हैं। ये दाँत
कृंतकों (rodent)
के दाँतों के
समान बराबर
बढ़ते रहते हैं
और इनका उपयोग
प्रहार करने
में होता है। चर्वण
दंत सरस खाद्य
खाने योग्य होते
हैं और घास,
टहनी जेसे रूखे
खाद्य खाने लायक
नहीं होते।
सुइडी
(Suidae)
- इनका
थूथन लंबा एवं
शंक्वाकार होता
है, जिनके चकतीनुमा
ऊर्ध्वाधर सिरे
पर चीरे से
नासारध्रं होते
हैं। इनका सिर
लंबा होता है,
आँख, कान छोटे
होते हैं और
मुँह मांसभक्षियों
की तरह चीरा
(cleft) होता
है। इनमें दाँतों
का पुरा समूह
(set) होता
है, काटनेवाले
निचले दाँत बाहर
की ओर उभरे
होते हैं और
नर के बड़े बड़े भेदक
दाँत (canines)
हाथी के दाँत
के समान मुँह
के बाहर निकले
होते हैं। ये दाँत
कृंतकों (rodent)
के दाँतों के
समान बराबर
बढ़ते रहते हैं
और इनका उपयोग
प्रहार करने
में होता है। चर्वण
दंत सरस खाद्य
खाने योग्य होते
हैं और घास,
टहनी जेसे रूखे
खाद्य खाने लायक
नहीं होते।
सूअर
सर्वभक्षी हैं। मांस
तथा घास, शाक,
फल आदि वानस्पतिक
खाद्य ये बेरोक
खाते हैं। इनके
अग्रपाद खाने तथा
खाद्य को पकड़ने
में सहायक होते
हैं। त्वचा पतली
और शूकयुक्त
(bristly) होती
है। बच्चे धारीदार
हेते हैं। ये फसलों
को बहुत हानि
पहुँचाते हैं,
पानी और कीचड़
में लोटना पसंद
करते हैं। नर
सूअर कभी कभी
बड़े खतरनाक
साबित होते
हैं। भारत में सूअर
की केवल तीन
जातियाँ पाई
जाती हैं : भारतीय
जंगली सूअर (दक्षिण
भारतीय), पट्टित
सूअर (sus vittatus)
तथा क्षुद्र सूअर
(pigmy hog)*
 हिप्पोपोटैमिडी
(Hippopotamidae)
- हिप्पोपोटैमस
को दरियाई
घोड़ा भी कहते
हैं। इसका शरीर
और विशेषत:
पैर बहुत मजबूत
होते हैं, त्वचा
भारी तथा विरल
रोमयुक्त होती
हैं, यह तैरने
में कुशल होता
है और जलीय
पौधों पर निर्वाह
करता है। उभयचर
हिप्पोपोटैमस
लगभग १२ फुट लंबा
होता है। यह
नील नदी में और
उसके दक्षिण भाग
में अफ्रीका में पाया
जाता है। कीरोप्सिस
लाइबेरियन्सिस
(Choeropsis Liberiensis, pigmy hippo)
उभयचर हिप्पोपोटैमस
से छोटा होता
है और पश्चिम
अफ्रीका में पाया
जाता है।
हिप्पोपोटैमिडी
(Hippopotamidae)
- हिप्पोपोटैमस
को दरियाई
घोड़ा भी कहते
हैं। इसका शरीर
और विशेषत:
पैर बहुत मजबूत
होते हैं, त्वचा
भारी तथा विरल
रोमयुक्त होती
हैं, यह तैरने
में कुशल होता
है और जलीय
पौधों पर निर्वाह
करता है। उभयचर
हिप्पोपोटैमस
लगभग १२ फुट लंबा
होता है। यह
नील नदी में और
उसके दक्षिण भाग
में अफ्रीका में पाया
जाता है। कीरोप्सिस
लाइबेरियन्सिस
(Choeropsis Liberiensis, pigmy hippo)
उभयचर हिप्पोपोटैमस
से छोटा होता
है और पश्चिम
अफ्रीका में पाया
जाता है।
कैमेलिडी
(Camelidae)
- इस कुल
के प्राणियों के
पैर कोमल और
चौड़े होते हैं,
खुर नहीं होते,
एक जोड़ा छेदक
दंत होते हैं,
भेदक (canine)
दंत छोटे होते
हैं, या होते ही
नहीं। आमाशय में
तीन या चार
कक्ष होते हैं, जिनमें
से पहले दो कक्षों
में जलसंग्रह कोशिकाएँ
होती हैं। इनके
कूबड़ का अधिकांश
वसानिर्मित होता
है और आहार
की कमी होने
पर शरीर पोषण
में खप जाता है।
तीव्रगामी ऊँट
या साँडनी (dromedary)
के कूबड़ अल्पविकसित
होता है। इनका
निर्वाह स्थूल
वनस्पतियों पर
होता है। यौन
उत्तेजन के समय
नर बर्बर 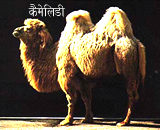 हो
जाते हैं और
तालु को लाल
गुब्बरे के समान
फुला लेते हैं।
मांसभक्षियों
की तरह, किंतु
खुरीय प्राणियों
के विपरीत, ये
अपने अंगों को
समेट कर ठीक
प्रकार से लेट
जाते हैं। इनकी
कुछ जातियाँ
निम्नलिखित हैं
: (१) कैमेलस बैक्ट्रियानस
(Camelus Bactrianus)
एशिया का दो
कूबड़वाला ऊँट
तथा (२) कैमेलस
ड्रोमेडेरियस
(Camelus Dromedarius)
अफ्रीका, एशिया तथा
उत्तर भारत का
एक कूबड़वाला ऊँट
तथा (३) लामा (Llama)
और अल्पाका (Alpaca),
जो पश्चिमी दक्षिण
अमरीका में पाए
जाते हैं और
परिवहन, मांस,
चमड़ा और ऊन
के काम आते हैं।
हो
जाते हैं और
तालु को लाल
गुब्बरे के समान
फुला लेते हैं।
मांसभक्षियों
की तरह, किंतु
खुरीय प्राणियों
के विपरीत, ये
अपने अंगों को
समेट कर ठीक
प्रकार से लेट
जाते हैं। इनकी
कुछ जातियाँ
निम्नलिखित हैं
: (१) कैमेलस बैक्ट्रियानस
(Camelus Bactrianus)
एशिया का दो
कूबड़वाला ऊँट
तथा (२) कैमेलस
ड्रोमेडेरियस
(Camelus Dromedarius)
अफ्रीका, एशिया तथा
उत्तर भारत का
एक कूबड़वाला ऊँट
तथा (३) लामा (Llama)
और अल्पाका (Alpaca),
जो पश्चिमी दक्षिण
अमरीका में पाए
जाते हैं और
परिवहन, मांस,
चमड़ा और ऊन
के काम आते हैं।
 मुंडि
कुल (Tragulidae)
मातृका मृग
(Chevrotains or Mouse deer)
- इस कुछ
के सदस्यों के
आमाशय में तृतीय
आमाशय या ओमेसम
(omasum) कक्ष
नहीं होता। संरचना
की दृष्टि से ये
सूअर और ऊँट
से काफी समानता
रखते हैं। भारतीय
मातृका मृग
(Indian chevrotains) दक्षिण
भारत और लंका
में पाए जाते हैं।
ये ऊँटों के समान
लेटते हैं। ये अकेले
घूमते हैं तथा
छिपने वाले (secretive)
और वनवासी
होते हैं। मादा
एक बार में एक या
दो बच्चों को
जन्म देती हैं।
मुंडि
कुल (Tragulidae)
मातृका मृग
(Chevrotains or Mouse deer)
- इस कुछ
के सदस्यों के
आमाशय में तृतीय
आमाशय या ओमेसम
(omasum) कक्ष
नहीं होता। संरचना
की दृष्टि से ये
सूअर और ऊँट
से काफी समानता
रखते हैं। भारतीय
मातृका मृग
(Indian chevrotains) दक्षिण
भारत और लंका
में पाए जाते हैं।
ये ऊँटों के समान
लेटते हैं। ये अकेले
घूमते हैं तथा
छिपने वाले (secretive)
और वनवासी
होते हैं। मादा
एक बार में एक या
दो बच्चों को
जन्म देती हैं।
जिराफ
कुल (Giraffidae)
- अफ्रीका में पाए
जानेवाले इस
कुल के जिराफ
की गर्दन तथा
पैर बहुत लंबे
होते हैं। चित्रोष्ट्र
(Camelopardalis)
१८ से २० फुट तक लंबा
होता है। इसके
सिर पर तीन
से पाँच तक त्वचावेष्टित
सींग होते हैं।
यह छुई मुई और
अन्य पेड़ों की पत्तियाँ
खाकर निर्वाह
करता है। ओकापिया
(Ocapia) अपेक्षाकृत
छोटा होता
है और इसकी
गर्दन भी छोटी
होती है।
 मृग
कुल (Cervidae)
- इस कुल
में मृग, वाहमृग
(reindeer),
वाहकुरंग (caribou)
आदि सम्मिलित
हैं। नर मृग को
ठोस चूर्णमय
(अस्थिमय) दो शृंगाभ
(antlers) होते
हैं, जो हर साल
झड़ते हैं और उनकी
जगह पर नए उग आते
हैं। इसकी निम्नलिखित
जातियाँ हैं :
मृग
कुल (Cervidae)
- इस कुल
में मृग, वाहमृग
(reindeer),
वाहकुरंग (caribou)
आदि सम्मिलित
हैं। नर मृग को
ठोस चूर्णमय
(अस्थिमय) दो शृंगाभ
(antlers) होते
हैं, जो हर साल
झड़ते हैं और उनकी
जगह पर नए उग आते
हैं। इसकी निम्नलिखित
जातियाँ हैं :
-
कस्तूरी
मृग (Musk deer)
- यह
पर्वतीय पशु
है तथा मध्य एशिया,
साइबीरिया
और ८,०००- १२,००० फुट
से अधिक ऊँचाई
पर हिमालय
और तिब्बत में
पाया जाता है।
यह केवल दो
फुट लंबा होता
है और सभी
मृगों में छोटा
है। इसके सींग
नहीं होती तथा
आवरण मोटा
और रूखे बालों
से युक्त होता
है। इसकी सादी
दुम दो इंच लंबी
होती है। इसके
पेट के नीचे
की एक थैली में
कस्तूरी होती
है। इसका रंग
निश्चित नहीं है।
�
कस्तूरी
मृग खरगोश
के समान असामाजिक
प्राणी है और
सदा अपनी माँद
में पड़ा रहता
है। ढालू स्थानों
पर यह आड़ में रहता
है। पैरों की
विचित्र बनावट
के कारण यह
चौकड़ी भरता
हुआ चलता है।
घासपात, फूल
एवं काई पर यह
निर्वाह करता
है। यह प्रजननकुशल
पशु है। एक वर्ष
की उम्र में ही यह
गर्भ-धारण-योग्य
हो जाता है।
इसके मांस में
कस्तूरी का स्वाद
नहीं होता। कस्तूरी
का व्यापार सदियों
पुराना धंधा
है। इसकी गंध
बहुत तेज होती
है और यह सुगंधित
वस्तुओं और दवाओं
के निर्माण में
काम आती है।

शंबर
महामृग (Cervus
unicolour, sdamar)
- यह
दक्षिण भारत
और लंका के
पर्वतीय जंगलों
में पाया जाता
है तथा फुट ऊँचा,
तीन नोकवाले
शृंगाभों से
युक्त, भारी भरकम
हरिण है। इसे
मार पाना कठिन
हाता है। इसका
मांस कुछ घटिया,
लेकिन स्वादिष्ठ
होता है।
-
पृषत
महामृग (Cervus
axis, चित्तीदार
हरिण, चित्तल)
यह दक्षिण भारत
और लंका में
पाया जाता है।
नर मादा से
बड़ा होता है।
यह मृग हलके
लाल-भूरे रंग
का होता है
और इसके बदन
पर सफेद चित्तियाँ
होती हैं। इसकी
सींग तीन शाखाओंवाली
होती है। यह
गिरोह में रहता
है। इसका मांस
स्वादिष्ट होता
है और चमड़े
से गलीचे बनते
हैं।

शाखिशृंग
महामृग (Cervus
devanceli, बारासिंगा
या दलदली मृग)
- यह केवल
भारत में हिमालय
की तराई और
गंगा तथा सिंध
नदी के मैदानों
में पाया जाता
है। इसका सिर
लंबा और थूथन
सँकरा होता
है। इसकी मादा
का रंग नर की
अपेक्षा हलका होता
है। मृगछौने
पर सफेद चित्तियाँ
होती हैं। इसके
दो शृंगाभ
होते हैं, जिनपर
१२ नोकें होती
हैं। इसके कारण
इसका नाम बारासिंगा
पड़ा है। यह यूथचारी
है तथा घास खाता
है और गरमियों
में जलाशयों
के निकट रहता
है।
बोविडी
कुल (Bovidae)
- इस कुल
के नर और मादा
दोनों के सींग
खोखले होते
हैं। सींग युग्मिन,
शाखाहीन और
केराटिन (keratin)
से बने होते
हैं। ये ललाटास्थियों
के अस्थिमय क्रोड़
के आधार पर
धीरे धीरे और
लगातार बढ़ते
रहते हैं। कुछ
वंशों का वर्णन
निम्नलिखित है
:
-
अवि वंश,
भेड़ (Ovis
sheep) - ये
छोटी पूँछवाले
पशु हैं। इनकी
टाँग लंबी, खुर
सुगठित और
छोटे, सींग आधार
पर मोटे, शुंडाकार
और चापाकार
में सर्पिल (spiral)
के समान, बाहर
तथा नीचे की
ओर फैले होते
हैं। बकरी जैसी
भेड़ की दाढ़ी नहीं
होती और न
उसके समान दुर्गंध
ही।
भेड़ तेज
चलनेवाला पर्वतीय
पशु है। यह पहाड़ों
पर चढ़ने उतरने
में तेज है, घास
पात पर निर्वाह
करती है और
इसकी दृष्टि सूक्ष्म
तथा घ्राण शक्ति
तेज होती है।
इसका मांस स्वादिष्ठ
होता है। यह
निरापद पशु
है तथा इसके खुरों
के बीच ग्रंथि
गर्त (gland pits)
होते हैं। ओविस
ऐमान (Ovis ammon),
मध्य और उत्तरी
एशिया में हड़प्पा
भेड़ (Ovis vignei)
सिंध पंजाब और
मध्य एशिया में पाइ
जाती हैं।

छाग (Capra)
बकरी - यह
भेड़ जैसी होती
है। अंतर इतना
ही है कि इसमें
खुरों के बीच
ग्रंथिगर्त नहीं
होते और भेड़ों
की अपेक्षा इसकी
दुम लंबी होती
है। इसकी ठुड्डी
पर दाढ़ी होती
है तथा इसकी
घ्राणशक्ति तीव्र
होती है। भेड़ों
की अपेक्षा चाल
धीमी होती
है, किंतु यह चढ़ने
में भेड़ से तेज
होती है। मादा
का मांस नर
के मांस की अपेक्षा
अधिक स्वादिष्ठ होता
है। केप्रा मेगासिरोज
(Capra megaceros)
अफगानिस्तान के
पर्वतों पर
और केप्रा एग्राग्रस
(Capra oegragrus)
पश्चिम एशिया से
सिंध तक के ऊँचे
भूभागों में
पाई जाती हैं।
-
एण (Antelope,
कुरंग Gazelle)
- ये
खुले, सूखे भूभागों
में पाए जाते हैं
तथा ये बकरी
के आकार के,
आकर्षक एवं सुकुमार
होते हैं। इनकी
गर्दन और टाँगें
लंबी और पतली,
आँखें बड़ी और
काली होती
हैं। इनके सींगों
पर वलय होते
हैं तथा वे कुछ
पीछे और बाहर
की ओर मुड़े होते
हैं। मादा को
सींग प्राय: नहीं
होती। ये गिरोह
बनाकर रहते
हैं और काफी
तेज दौड़ते हैं।
इनका रंग बालू
के रंग के सदृश
बलुआ या बादामी
होता है। भारत
में इनकी निम्नलिखित
जातियाँ पाई
जाती हैं :
(क) भारतीय
कुरंग (gazelle)
या चिंकारा -
यह मध्यभारत
और मैसूर
में पाया जाता
है तथा (ख) नीलगाय
(पोर्टेंक्स पिक्टस,
portex pictus)
- भारत
में यह सर्वत्र खुले
भूभागों में
पाई जाती है,
पर यह उत्तर-पश्चिम
और मध्य भागों
में बहुतायत
से मिलती हैं।
यह बैर, आँवला
आदि की पत्तियों
और उनके फलों
पर निर्वाह करती
हैं।
-
गो वंश
(Bos) -
इस वंश
के पशुओं का
शरीर सुगठित
होता है और
जुगाली करनेवाले
अन्य पशुओं की अपेक्षा
इनकी दुम लंबी
हाती है। इनके
थूथन लंबा, नम
और निराकरण
होता है। नर
और मादा दोनों
को सींग होते
हैं, तथा चेहरे
या पैर पर
ग्रंथियाँ नहीं
होतीं। ये सभी
स्तनपायियों
में उत्कृष्ट हैं, अधिकतर
घास खाते हैं
और पानी तथा
नमक पसंद करते
हैं। इनकी कुछ
भारतीय जातियाँ
निम्नलिखित हैं
:
(क) भारतीय
गाय (Bos Indicus)
- यह
विविध रंगों
में पाया जानेवाला
यह पालतू पशु
है। इस जाति की
गाय यूरोपीय
गाय से इस दृष्टि
से भिन्न होती
है कि इसके सींग
यूरोपीय गायों
से कम फैले और
पीछे की ओर
अधिक मुड़े होते
हैं। इसके एक वसामय
कूबड़ भी होता
है। दूध देनेवाले
पशु के रूप में
यह अतिशय उपयोगी
है। अफ्रीका और
दक्षिण पूर्वी एशिया
पूर्वी एशिया में
यह सर्वत्र पाई
जाती है।
(ख) भैंस
(Bos bubalus)
- यह पूर्व
तथा मध्य भारत
के मैदानों में
पाई जाती है।
इसका माथा लंबा,
टाँग छोटी, खुर
बड़े, पीठ सीधी,
पिछले घुटनों
को छूती हुई
दुम, बाल पतले
और खुरदरे,
तथा उभरी हुई
रैखाओं से चिन्हित,
त्रिकोणाकार,
विचित्र सींग होता
है। पालतू भैंसे
का उपयोग कर्षक
पशु के रूप में होता
है। यह बहुत बलवान
पर मंद चालवाला
होता है। इसे
जल प्रिय है, प्राय:
गर्मियों में दिन
का समय पानी
में पड़े पड़े बिताता
है। दुग्ध पशु के
रूप में भैंस मूल्यवान
है।
(रामचंद्र
सक्सेना)
 सुइडी
(Suidae)
- इनका
थूथन लंबा एवं
शंक्वाकार होता
है, जिनके चकतीनुमा
ऊर्ध्वाधर सिरे
पर चीरे से
नासारध्रं होते
हैं। इनका सिर
लंबा होता है,
आँख, कान छोटे
होते हैं और
मुँह मांसभक्षियों
की तरह चीरा
(cleft) होता
है। इनमें दाँतों
का पुरा समूह
(set) होता
है, काटनेवाले
निचले दाँत बाहर
की ओर उभरे
होते हैं और
नर के बड़े बड़े भेदक
दाँत (canines)
हाथी के दाँत
के समान मुँह
के बाहर निकले
होते हैं। ये दाँत
कृंतकों (rodent)
के दाँतों के
समान बराबर
बढ़ते रहते हैं
और इनका उपयोग
प्रहार करने
में होता है। चर्वण
दंत सरस खाद्य
खाने योग्य होते
हैं और घास,
टहनी जेसे रूखे
खाद्य खाने लायक
नहीं होते।
सुइडी
(Suidae)
- इनका
थूथन लंबा एवं
शंक्वाकार होता
है, जिनके चकतीनुमा
ऊर्ध्वाधर सिरे
पर चीरे से
नासारध्रं होते
हैं। इनका सिर
लंबा होता है,
आँख, कान छोटे
होते हैं और
मुँह मांसभक्षियों
की तरह चीरा
(cleft) होता
है। इनमें दाँतों
का पुरा समूह
(set) होता
है, काटनेवाले
निचले दाँत बाहर
की ओर उभरे
होते हैं और
नर के बड़े बड़े भेदक
दाँत (canines)
हाथी के दाँत
के समान मुँह
के बाहर निकले
होते हैं। ये दाँत
कृंतकों (rodent)
के दाँतों के
समान बराबर
बढ़ते रहते हैं
और इनका उपयोग
प्रहार करने
में होता है। चर्वण
दंत सरस खाद्य
खाने योग्य होते
हैं और घास,
टहनी जेसे रूखे
खाद्य खाने लायक
नहीं होते। हिप्पोपोटैमिडी
(Hippopotamidae)
- हिप्पोपोटैमस
को दरियाई
घोड़ा भी कहते
हैं। इसका शरीर
और विशेषत:
पैर बहुत मजबूत
होते हैं, त्वचा
भारी तथा विरल
रोमयुक्त होती
हैं, यह तैरने
में कुशल होता
है और जलीय
पौधों पर निर्वाह
करता है। उभयचर
हिप्पोपोटैमस
लगभग १२ फुट लंबा
होता है। यह
नील नदी में और
उसके दक्षिण भाग
में अफ्रीका में पाया
जाता है। कीरोप्सिस
लाइबेरियन्सिस
(Choeropsis Liberiensis, pigmy hippo)
उभयचर हिप्पोपोटैमस
से छोटा होता
है और पश्चिम
अफ्रीका में पाया
जाता है।
हिप्पोपोटैमिडी
(Hippopotamidae)
- हिप्पोपोटैमस
को दरियाई
घोड़ा भी कहते
हैं। इसका शरीर
और विशेषत:
पैर बहुत मजबूत
होते हैं, त्वचा
भारी तथा विरल
रोमयुक्त होती
हैं, यह तैरने
में कुशल होता
है और जलीय
पौधों पर निर्वाह
करता है। उभयचर
हिप्पोपोटैमस
लगभग १२ फुट लंबा
होता है। यह
नील नदी में और
उसके दक्षिण भाग
में अफ्रीका में पाया
जाता है। कीरोप्सिस
लाइबेरियन्सिस
(Choeropsis Liberiensis, pigmy hippo)
उभयचर हिप्पोपोटैमस
से छोटा होता
है और पश्चिम
अफ्रीका में पाया
जाता है।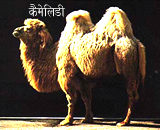 हो
जाते हैं और
तालु को लाल
गुब्बरे के समान
फुला लेते हैं।
मांसभक्षियों
की तरह, किंतु
खुरीय प्राणियों
के विपरीत, ये
अपने अंगों को
समेट कर ठीक
प्रकार से लेट
जाते हैं। इनकी
कुछ जातियाँ
निम्नलिखित हैं
: (१) कैमेलस बैक्ट्रियानस
(Camelus Bactrianus)
एशिया का दो
कूबड़वाला ऊँट
तथा (२) कैमेलस
ड्रोमेडेरियस
(Camelus Dromedarius)
अफ्रीका, एशिया तथा
उत्तर भारत का
एक कूबड़वाला ऊँट
तथा (३) लामा (Llama)
और अल्पाका (Alpaca),
जो पश्चिमी दक्षिण
अमरीका में पाए
जाते हैं और
परिवहन, मांस,
चमड़ा और ऊन
के काम आते हैं।
हो
जाते हैं और
तालु को लाल
गुब्बरे के समान
फुला लेते हैं।
मांसभक्षियों
की तरह, किंतु
खुरीय प्राणियों
के विपरीत, ये
अपने अंगों को
समेट कर ठीक
प्रकार से लेट
जाते हैं। इनकी
कुछ जातियाँ
निम्नलिखित हैं
: (१) कैमेलस बैक्ट्रियानस
(Camelus Bactrianus)
एशिया का दो
कूबड़वाला ऊँट
तथा (२) कैमेलस
ड्रोमेडेरियस
(Camelus Dromedarius)
अफ्रीका, एशिया तथा
उत्तर भारत का
एक कूबड़वाला ऊँट
तथा (३) लामा (Llama)
और अल्पाका (Alpaca),
जो पश्चिमी दक्षिण
अमरीका में पाए
जाते हैं और
परिवहन, मांस,
चमड़ा और ऊन
के काम आते हैं। मुंडि
कुल (Tragulidae)
मातृका मृग
(Chevrotains or Mouse deer)
- इस कुछ
के सदस्यों के
आमाशय में तृतीय
आमाशय या ओमेसम
(omasum) कक्ष
नहीं होता। संरचना
की दृष्टि से ये
सूअर और ऊँट
से काफी समानता
रखते हैं। भारतीय
मातृका मृग
(Indian chevrotains) दक्षिण
भारत और लंका
में पाए जाते हैं।
ये ऊँटों के समान
लेटते हैं। ये अकेले
घूमते हैं तथा
छिपने वाले (secretive)
और वनवासी
होते हैं। मादा
एक बार में एक या
दो बच्चों को
जन्म देती हैं।
मुंडि
कुल (Tragulidae)
मातृका मृग
(Chevrotains or Mouse deer)
- इस कुछ
के सदस्यों के
आमाशय में तृतीय
आमाशय या ओमेसम
(omasum) कक्ष
नहीं होता। संरचना
की दृष्टि से ये
सूअर और ऊँट
से काफी समानता
रखते हैं। भारतीय
मातृका मृग
(Indian chevrotains) दक्षिण
भारत और लंका
में पाए जाते हैं।
ये ऊँटों के समान
लेटते हैं। ये अकेले
घूमते हैं तथा
छिपने वाले (secretive)
और वनवासी
होते हैं। मादा
एक बार में एक या
दो बच्चों को
जन्म देती हैं। मृग
कुल (Cervidae)
- इस कुल
में मृग, वाहमृग
(reindeer),
वाहकुरंग (caribou)
आदि सम्मिलित
हैं। नर मृग को
ठोस चूर्णमय
(अस्थिमय) दो शृंगाभ
(antlers) होते
हैं, जो हर साल
झड़ते हैं और उनकी
जगह पर नए उग आते
हैं। इसकी निम्नलिखित
जातियाँ हैं :
मृग
कुल (Cervidae)
- इस कुल
में मृग, वाहमृग
(reindeer),
वाहकुरंग (caribou)
आदि सम्मिलित
हैं। नर मृग को
ठोस चूर्णमय
(अस्थिमय) दो शृंगाभ
(antlers) होते
हैं, जो हर साल
झड़ते हैं और उनकी
जगह पर नए उग आते
हैं। इसकी निम्नलिखित
जातियाँ हैं :

