 है।
है।चुंबकत्वमापी सामान्य अर्थ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने का एक उपकरण है, पर संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज अवयव को मापने में ही बहुधा होता है। इसी अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है और कुछ चुंबकत्वमापियों के सिद्धांत दिए जा रहे हैं।
पहला चुंबकत्वमापी, जिसका प्रयोग आज भी प्राय: उसी रूप में हो रहा है, गौस ने १९३२ ई. में तैयार किया था। यह एक निरपेक्ष उपकरण है, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबक का चुंबकीय घूर्ण भी मापा जा सकता है। पहले ऐंठनहीन सूत्र द्वारा चुंबक को चुंबकीय दोलक के रूप लटकाते हैं। चुंबक को साम्यावस्था से अल्प विचलित करने पर चुंबक पर
2 m 1 H sin q = M H sin q MH q
परिमाण में बलयुग्म कार्य करता है। समीकरण में M चुंबक का चुंबकीय घूर्ण, H पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव और q अल्प होने पर sin q = q । यदि चुंबक का जड़ताघूर्ण I हो, ते घूर्णन गति का समीकरण-
![]() =
M H q
और हल
q = A
sin
=
M H q
और हल
q = A
sin  है।
है।
A, B स्थिरांक हैं और प्रारंभिक प्रतिबंधों से इनका मान ज्ञात हो सकता है। यह हल आवर्त गति का प्रतिनिधित्व करता है। q का यही मान T इसके बाद इस प्रकार पुनरावृत्त होता है कि
A sin 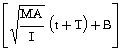
=
A sin 
या ![]() अर्थात्
अर्थात्
![]()
कुछ दोलनों का समय देखकर T का मान निकाल लेते हैं। I चुंबक के द्रव्यमान ओर परिमाप पर निर्भर करता है और गणना द्वारा ज्ञात हो सकता है। अत:
![]() ..................... (१)
..................... (१)
अब इसी चुंबक से दिक्सूचक को विचलित करते हैं। कल्पना कीजिए, सुई एक बिंदु पर है और उत्तर-दक्षिण दिशा में साम्यावस्था में स्थित है। कंपन प्रयोग में प्रयुक्त चुंबक से उपर्युक्त बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत् क्षेत्र उत्पन्न करने पर दिक्सूचक q कोण पर विचलित हाता है और दोनों बलयुग्म आपस में संतुलित हो जाते हैं, अर्थात् FM Cosq =HM sinq , या F=H tanq ।
प्रदर्शित स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
![]()
होता
है। अत: ![]()
या ![]() .........................................(२)
.........................................(२)
विचलन को परिशुद्धतापूर्वक मापने के लिये दिक्सूचक सुई के लंबवत् एक हलका और लंबा संकेतक लगा होता है। प्रयोग में संभव त्रुटियों को कम करने के लिये संकेतक के दोनों सिरों के आठ पठनों का औसत लेते हैं। ये पठन, चुंबक को प्रदर्शित स्थिति में रखकर दिक्सूचक के उसी ओर चुंबक के सिरों को प्रतिवर्तित करके, फिर चुंबक को दिक्सूचक के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर रख तथा प्रयोग दोहराकर, लिए जाते हैं।
समीकरण (१) और (२) से गुणा तथा भाग करने पर क्रमश: M और H का मान प्राप्त होता है। प्रयोगशाला के उपकरण की यथार्थता ३- ४ g (g = १०- ५ ओस्टेंड) और इसके क्षेत्र उपकरण की यथार्थता लगभग ८ g है। उपकरण का मुख्य दोष यह है कि प्रयोग में लगभग एक घंटे का लंबा समय लगता है।
H का मान ज्ञात करने की दूसरी विधि में हेल्महोल्ट्ज कुंडलीवाले ज्या धारामापी का प्रयोग होता है। हेल्महोल्ट्ज कुंडली में दो समरूप, समाक्ष कुंडलियाँ एक दूसरे से अर्धव्यास की आधी दूरी पर रखी होती हैं। यदि कुंडलियों का अर्धव्यास r और उसमें प्रवहित धारा i विद्युच्चुंबकीय इकाई हो तो मध्य बिंदु पर
 क्षेत्र उत्पन्न
होगा। मध्य बिंदु
पर यदि चुंबकीय
सुई रखी जाय,
तो वह धारामापी
में प्रवाहित धारा
से उत्पन्न एक सम क्षेत्र
में होगी। यदि
कुंडली तंत्र को
पार्थिव चुंबकीय
क्षेत्र में इस प्रकार
घूर्णित किया
जाय कि सुई कुंडलियों
के समतल के समांतर
हो और धारा
काट दी जाय, तो
सुई का विचलन
ज्ञात हो जाता
है। साम्यावस्था
के प्रतिबंध से-
क्षेत्र उत्पन्न
होगा। मध्य बिंदु
पर यदि चुंबकीय
सुई रखी जाय,
तो वह धारामापी
में प्रवाहित धारा
से उत्पन्न एक सम क्षेत्र
में होगी। यदि
कुंडली तंत्र को
पार्थिव चुंबकीय
क्षेत्र में इस प्रकार
घूर्णित किया
जाय कि सुई कुंडलियों
के समतल के समांतर
हो और धारा
काट दी जाय, तो
सुई का विचलन
ज्ञात हो जाता
है। साम्यावस्था
के प्रतिबंध से-
mF.21=mH 21 sinq , या F=H sinq ।
इस प्रकार H का मान कुंडली के स्थिरांक और विचलन में प्राप्त होता है। मापन में कुछ ही मिनट लगते हैं और यथार्थता लगभग ०.५g होती है।
प्रोटॉन चुंबकत्वमापी स चुंबकीय तीव्रता प्रोटॉन के ज्ञात न्यूक्लीय चुंबकीय घूर्ण में प्राप्त होती है। यह उपकरण पार्थिव क्षेत्र के असमांतर साधारण मंद क्षेत्र द्वारा प्रोटॉन को द्रव में संरेखित करता है। प्रोटॉन दिक्स्थापित होकर मंद क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ध्रुवण क्षेत्र (polarizing field) सहसा काट दिया जाता है। जो न्यूक्लीय चुंबकीय घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में संरेख्ति हुए थे, वे अब पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर अयन (precess) करते हैं। अयन की आवृत्ति क्षेत्र की अनुपाती होती है। संरेखण शीघ्र टूटता है, पर उपयुक्त माध्यम में कुछ सेंकड तक बना रहता है। बेंजीन में २० सेंकड तक संरेखण नष्ट नहीं होता। अयनकारी प्रोटॉन द्वारा किसी कुंडली में प्रेरित वोल्टता से अयन की अवृत्ति का निर्धारण होता है। उपकरण की यथार्थता लगभग ०.५g है। इसकी सबसे मुख्य विशेषता यह है कि प्रयोग में समय बहुत ही कम लगता है। कुछ सेकंडों में ही प्रयोग पूरा हो जाता है। स्थानीय चुंबकीय सर्वेक्षणों में प्रोटॉन चुंबकत्वमापी बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं।
स्थान या काल के अनुसार पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित परिवर्तन जानना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। इसके लिये सापेक्ष चुंबकत्वमापी का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष चुंबकत्वमापी में स्फटिक अनुप्रस्थ चुंबकत्वमापी (quartz horizontal magnetometer) का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसका अभिकल्पन १९३६ ई. में लाकूर (Lacour) ने किया था। M चुंबकीय घूर्ण के चुंबक को T ऐंठन स्थिरांक के स्फटिक तॉतवक से लटकाया जाता है। माना चुंबक चुंबकीय याम्योत्तर से a कोण बनाता है और स्फटिक तांतवक में अवशिष्ट ऐठन d है। २p और - २p ऐंठन पर क्रमश: a + f १ और a - f २ पठन प्राप्त होते हैं। इन कोणों को तब पढ़ते हैं जब सिरे को घूर्णित करने पर स्थिति के सापेक्ष चुंबक पुन: उसी स्थिति में होता है। अत:
MH Sin a = Td ; MH sin (a + F 1)=T (d + 2 p ) और MH sin (a - f 2 )=T(d - 2 p )
ऐंठनदार स्थितियों में प्राप्त पठनों का अंतर 2 q = f 1 + f 2 है। इसे हम यों परिभाषित करते हैं : f 1 - f 2 = 2 b अब और के अल्प मान के लिये
H=2p T/M sinq [1 - b 2 / { 2 ( 1 - Cosq ) 2 } ] और a = b Cos q / ( 1 - cosq )
अत: यदि T/M का मान ज्ञात हो तो H का मान निर्धारित किया जा सकता है। T/M ताप पर निर्भर करता है, अत: ताप के मापने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस सिद्धांत पर बने युंबकत्वमापी क्षेत्रप्रेक्षण के लिये बहुत लाभदायक हैं और इनका व्यापक प्रयोग होता है।
सं.ग्रं. - जे. थ्यूलिस द्वारा संपादित : इनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑवृ फिज़िक्स, परगामन प्रेस (१९६१); एस.के. रंकॉर्न द्वारा संपादित : मेथड्स ऐंड टेकनीक्स इन जियोफिज़िक्स, प्रथम भाग, इंटर सायंस पब्लिशर्स (१९६०)। (शिवयोगी तिवारी)