- ईसा की
मृत्यु के बाद
उनके शिष्य यहूदियों
तथा गैर यहूदियों
में ईसाई धर्म
का प्रचार करने
लगे। प्रथम मिशनरियों
में से सबसे सफल
थे संत पौलुस;
उनकी यात्राओं
का वर्णन तथा
उनके पत्र बाईबिल
के उत्तरार्ध में
सुरक्षित हैं।
उस समय अंतिओक
(Antioch)
रोमन साम्राज्य
का तीसरा शहर
था, ईस का उत्तराधिकारी
संत पेत्रुस यहीं
चले आए और उस
केंद्र से संत पौलुस
ने एशिया माइनर,
मासेदोनिया
तथा यूनान में
ईसाई धर्म का
प्रचार किया।
बाद में राजधानी
रोम ईसाई
धर्म का प्रधान
केंद्र बना। वहीं
संत पेत्रुस (६७ ई.)
और संत पौलुस
शहीद हो गए। बाइबिल
का उत्तरार्ध प्रथम
शताब्दी ई. के
उत्तरार्ध में लिखा
गया (दे. ''बाइबिल'')
सन् १०० ई. तक भूमध्यसागर
के सभी निकटवर्ती
देशों और नगरों
में, विशेषकर
एश्यि माइनर तथा
उत्तर अफ्रीका में
ईसाई समुदाय
विद्यमान थे। तीसरी
शताब्दी के अंत
तक ईसाई धर्म
विशाल रोमन
साम्राज्य के सभी
नगरों में फैल
गया था; इसी समय
फारस तथा दक्षिण
रूस में भी बहुत
से लोग ईसाई
बन गए। इस सफलता
के कई कारण
हैं। एक तो उस समय
लोगों में प्रबल
धर्मजिज्ञासा
थी, दूसरे ईसाई
धर्म प्रत्येक मानव
का महत्व सिखलाता
था, चाहे वह दास
अथवा स्त्री ही क्यों
न हो। इसके अतिरिक्त
ईसाइयों में
जो भातृभाव
था उससे लोग
प्रभावित हुए बिना
नहीं रह सके।
- प्रथम तीन
शताब्दियों के
इतिहास की सबसे
बड़ी विशेषता
यह है कि समय
पर शासकों
द्वारा ईसाइयों
पर अत्याचार
किया गया और
वे बड़ी संख्या में
अपना धर्म छोड़
देने की अपेक्षा
सानंद यंत्रणा
एवं मृत्यु स्वीकार
करते थे। यद्यपि
रोमन शासक
प्रारंभ ही से
उस नए धर्म को
संदेह की दृष्टि
से देख्ते थे और
उसके अनुयायियों
को सताते थे,
फिर भी केवल
तीसरी शताब्दी
में ईसई धर्म
को पूर्ण रूप
से मिटाने का
ध्यापक प्रयत्न किया
गया था, विशेष
रूप से देसियस,
डाइयोक्लीशन
(Diocletian),
मस्किमिनियन
और गालेरियस
के शासनकाल
में (तीसरी के
उत्तरार्ध तथा
चतुर्थ शताब्दी
के प्रारंभ में)।
- संगठन
इस प्रकार था
: हर शहर में
स्थानीय गिरजे
का परमाधिकारी
धर्माध्यक्ष (बिशप)
कहलाता था, उनके
शासन में पुरोहित
(याजक) और उपपुरोहित
(उपयाजक या डीकन)
धर्म कार्यो में
लगे रहते थे।
रोम, सिकंदरिय,
अंतिओक (और
बाद में कुछ और
महत्वपूर्ण शहरों)
में बिशपों को
पेत्रिआर्क (Patriarch)
की उपाधि दी जाती
थी किंतु सर्वत्र
रोम के बिशप
का विशेष अधिकार
माना जाता था।
- प्रारंभिक
ईसाई साहित्य
प्रधानतया यूनानी
भाषा में लिखा
गया है। ओरिजेन
(दे. ओरिजेन)
और संत इरेनेयस
विशेष रूप से
उल्लेखनीय हैं। इरेनेयस
(१३०-२०२ ई.) ने तत्कालीन
भ्रामक धारणाओं
का विरोध करते
हुए रोमन चर्च
की शिक्षा को
सच्ची ईसाई शिक्षा
की कसौटी घोषित
किया। उन्होंने
अधिकतर ईसाई
गूढ़ज्ञानवाद
(Gnosticism)
का खंडन किया।
गूढ़ज्ञानवाद
ईसा के पूर्व
ही से चला आ रहा
था किंतु बाद
में इसमें ईसाई
तत्वें का समावेश
किया गया था।
उस वाद का मूलभूत
सिद्धांत है कि
समस्त भौतिक
जगत् और मानवशरीर
भी दूषित है।
किसी न किसी
रूप में यह सिद्धांत
शताब्दियों तक
जीवित रहा।
(दे. नीचे अनु. १४)
उत्तरी अफ्रीका
के निवासी तेरतुलियन
(Tertullian
१६०-२२० ई.) लैटिन भाषा
के प्रथम विख्यात
ईसाई लेखक
हैं। दूसरी शताब्दी
के अंत तक एदेस्सा
के आसपास सिरियक
भाषा में ईसाई
साहित्य की रचना
प्रारंभ हो गई
थी।
(आ) रोमन साम्राज्य
के संरक्षण में
(३१३-७५० ई.)
- डाइयोक्लीशन
के पदत्याग के
बाद उत्तराधिकारी
के लिये जो
गृहयुद्ध हुआ
उसमें कोंस्तांतीन
विजयी हुआ और
उसने ३१३ ई. में मिलान
की राजाज्ञा
(Edict of Milan)
निकालकर सभी
धर्मो को स्वतंत्रता
प्रदान कर दी।
उस समय आरियस
के मत के कारण
ईसाई संसार
में अशांति फैलने
लगी थी। उसे दूर
करने के उद्देश्य
से कोंस्तांतीन
ने कॉथलिक
चर्च की प्रथम
विश्वसभा का आयोजन
किया; नीकिया
(३१५ ई.) की इस सभा
ने ऑरियस
के मत के विरोध
में घोषित किया
कि ईसा वास्तविक
अर्थ में ईश्वर हैं
(दे. ऑरियस)।
कोंस्तांतीन
के उत्तराधिकारियों
ने आरियस के
अनुयायियों
का पक्ष लिया,
फलस्वरूप लगभग
५० वर्ष तक पूर्वी
काथलिक चर्च
में इतनी अव्यवस्था
रही कि वहाँ
का चर्च उस कुप्रभाव
से कभी मुक्त नहीं
हो पाया। उस शताब्दी
के अंत में प्रथम
वास्तविक ईसाई
सम्राट् थेओदोसियस
(Theodosius)
ने ईसाई धर्म
को राजधर्म
के रूप में घोषित
किया; उन्होंने
ऑरियस के
अनुयायियों
का नियंत्रण भी
किया और उस
उद्देश्य से कुंस्तुंतुनिआ
(३८१ ई.) में काथलिक
चर्च की द्वितीय
विश्वसभा का आयोजन
किया।
पाँचवीं शताब्दी
में और दो
बार विश्वसभा
बुलाई गई। कुंस्तुंतुनिआ
का बिशप नेस्तोरियस
एक नए सिद्धांत
का प्रचार करने
लगा जिसके अनुसार
ईसा में ईश्वरीय
और मानवीय
दो व्यक्ति विद्यमान
थे। एफेसस (४३१ ई.)
की विश्वसभा ने
नेस्तोरियस
को पदच्युत किया
और उसके अनुयायियों
को चर्च से बहिष्कृत
घोषित किया,
इसके फलस्वरूप
फारस का चर्च
अलग हो गया। बाद
में युतिकेस
ने मोनोफिजितिज्म
(एकस्वभाववाद)
का प्रवर्तन किया
जिसके अनुसार
ईसा में एक ही
व्यक्ति और एक ही
स्वभाव है। इस मत
के विरोध में
कालसेदोन
(४५१ ई.) की विश्वसभा
ने ईसा में ईश्वरत्व
तथा मनुष्यत्व
दोनों को
वास्तविक माना
है। सीरिया,
आरमीनिया
और मिस्त्र के
बिशपों ने कालसेदोन
के निर्णय को
अस्वीकार किया
और उन देशों
के ईसाई समुदाय
भी काथलिक चर्च
से अलग हो गए (आजकल
भी एथियोपिया
के ईसाई और
दक्षिण भारत
के जैकोबाइट
मोनोफीसाइट
हैं)। बाद में इस्लाम
ने सीरिया और
मिस्त्र को साम्राज्य
से छीन लिया
और वहाँ के
अधिकांश लोग
उस नए धर्म से सम्मिलित
हुए।
- इस युग के प्रारंभ
में ईसाई सहित्य
का अपूर्व विकास
हुआ। यूनानी
भाषा के लेखकों
में अथानासियस
(२९५-२७३ ई.), संत बासिल
(३२१-३७९ ई.) और उनके
भाई निस्सा के
संत ग्रेगोरी
(३३५-३९५ ई.), नाजिअंसस
के संत ग्रेगोरी
(३३०-३९०), कुंस्तुंतुनिया
के बिशप संत
योहन क्रिसोस्तेमस
(३४७-४०४) और सिकंदरिया
के संत सीरिलस
(३८०-४४४) विशेष रूप से
उल्लेखनीय हैं।
पश्चिम में लैटिन
भाषा के मुख्य
ईसाई लेखक
इस प्रकार हैं :
मिलान के बिशप
संत अंब्रोसियस
(३४०-३९९ ई.), संत अगस्तिन
(३५४-४३० ई.) और सत
जेरोम (३४७-४२०)। संत
जेरोम ने समस्त
बाइबिल का लैटिन
भाषा में अनुवाद
किया और उनका
अनुवाद आज तक
रोमन चर्च
की पूजापद्धति
में प्रयुक्त है।
- ईसाई धर्म के
प्रारंभ से ही
कुछ लोग आजीवन
ब्रह्मचारी रहने
का व्रत लेते थे,
वे बहुधा निर्जन
स्थानों में रहकर
एकांतवासी होते
थे किंतु धीरे
धीरे उनके पड़ोस
में उनके शिष्य भी
उनके निर्देश के
अनुसार साधना
करने लगे। इसका
परिणाम यह
हुआ कि एक ही स्थान
में रहनेवाले
साधकों ने एक
ही अधिकारी
का शासन स्वीकार
कर लिया। इस
प्रकार के प्रथम
मठ की स्थापना
लगभग ३२० ई. में
संत पाकोमियस
द्वारा मिस्त्र में
हुई थी। इसके
अनुकरण पर फिलिस्तीन,
सीरिया और
एशिया माइनर
में बड़ी संख्या
में पुरुषों और
स्त्रियों के मठों
की स्थापना हुई
थी और पाँचवीं
शताब्दी में सिकंदरिया,
आंतिओक, कुंस्तुंतनिया
आदि शहरों
में भी ऐसे मठ
स्थापित हो चुके
थे। उनमें प्राय:
संत बासिल की
नियमावली स्वीकृत
थी।
पश्चिम में संत
मारतिन ने
पहले पहल ३६० ई.
में फ्रांस के दक्षिण
में एक मठ स्थापित
किया गया और
उसी केंद्र से फ्रांस
के सभी देहातों
में ईसाई धर्म
का प्रचार हुआ
क्योंकि उस समय
तक केवल इटली
तथा उत्तर अफ्रीका
का देहात ईसाई
बन गया था। संत
पैत्रिक (३९२-४६१ ई.) पहले
फ्रांस में मठवासी
थे, उन्होंने अपने
शिष्यों के साथ
आयरलैंड को
ईसाई धर्म में
मिला लिया और
बाद में वहाँ
के संन्यासियों
ने बड़ी संख्या में
पश्चिम यूरोप
के देशों (विशेषकर
दक्षिण जर्मनी,
स्विट्जरलैंड,
दक्षिण बेलजियम)
में ईसाई धर्म
का प्रचार किया।
संत बेनेदिक्त
(४८०-५४७) ने भी एक धर्मसंघ
की स्थापना की
और मठवासी
जीवन के लिये
एक नियमावली
लिखी जिसे यूरोप
के प्राय: सभी मठों
ने स्वीकार कर
लिया। बेनेदिक्ताइन
संघ के संन्यासी
ईसा की छठी
शताब्दी में इंग्लैंड
भेजे गए (जहाँ
बर्बर जातियों
के आगमन से कम
ईसाई रह गए
थे)। उन्होंने वहाँ
की जातियों
को ईसाई धर्म
में मिला लिया
और अपने संघ
के मठ भी स्थापित
किए। संत बीड (६७२-७३५
ई.) एक अंग्रेज बेनेदिक्ताइन
थे जिन्होंने
इंग्लैंड का सर्वप्रथम
इतिहास लिखा।
एक समकालीन
अंग्रेज बेनेदिक्ताइन
संत बोनिफास
(६७५-७५५) ने पहले हालैंड
में धर्मप्रचार
किया और बाद
में जर्मनी के
अधिकांश भाग
को ईसाई धर्म
में मिलाया। पश्चिम
में ईसाई धर्म
के इस प्रचार का
श्रेय मुख्य रूप से
मठवासियों
को ही है।
- पाँचवीं
शताब्दी से पश्चिम
रोमन साम्राज्य
तथा उत्तर अफ्रीका
में बर्बर जातियों
का आगमन प्रारंभ
हुआ था ओर उस
शताब्दी के अंत
में इटली के बाहर
सर्वत्र उन बर्बर
राजाओं का
शासन स्थापित
हो चुका था।
उनमें से एक भी
काथलिक नहीं
था। ४९६ ई. में फ्रैंक
(Frank)
जाति के राजा
क्लोविस ने ईसाई
धर्म स्वीकार
किया। छठी शताब्दी
के अंत में काथलिक
फ्रैंक जाति ने
समस्त वर्तमान
फ्रांस देश पर
अधिकार कर लिया।
पुर्तगाल की
सुएवी (Suevi)
जाति भी छठी
शताब्दी के मध्य
काथलिक धर्म
में सम्मिलित हो
गई और स्पेन
के विजीगोथ
(Visigoth)
५८९ ई. में ऑरियस
का मत त्याग कर
काथलिक बन गए।
अगली शताब्दी
में स्पेन के सबसे
महत्वपूर्ण् ऐतिहासिक
व्यक्ति संत इसीदोर
(Isidore)
हैं जो ३६ वर्ष तक
(६००-६३६ ई.) सेविल के
बिशप थे।
- संत ग्रेगोरी
५९० ई. में रोम
के बिशप (पोप)
चुने गए। उनके शासनकाल
में इटली पर लोंबार्द
जाति का आक्रमण
हुआ। सम्राट्
उनका विरोध
करने में असमर्थ
था और संत
ग्रेगारी ने लोंबार्द
नेताओं से भेंट
कर रोम की
रक्षा की। वास्तव
में वह उस समय
रोम के वास्तविक
शासक थे। उन्हीं
को कॉथलिक
चर्च के राज्य
(पेपल स्टेट्स)
का संस्थापक माना
जा सकता है।
संत ग्रेगोरी
के जीवनकाल
में हजरत मुहम्मद
का जन्म हुआ था;
उनके अनुयायी
६९५ ई. में उत्तर अफ्रीका
तथा ७११ ई. में स्पेन
पर अधिकार कर
लिया। यद्यपि पूर्व
में कुंस्तुंतुनिया
का अवरोध (७१७ ई.)
असफल हुआ तथा
पश्चिम में फ्रैक
जाति के चार्ल्स
मारतेल ने मुसलमान
सेनाओं को
फ्रांस के दक्षिण
में (Poitiers;
७३२ ई.) हरा दिया
था, तथापि उस
समय से लेकर
९०० वर्ष तक ईसाई
तथा मुसलमान
सेनाओं का संघर्ष
चलता रहा।
चार्ल्स मारतेल
का पुत्र पेपीन
फ्रैंक जाति का
राजा बन गया।
कुछ समय बाद
इटली पर लोंबार्द
जाति का नया
आक्रमण हुआ। सम्राट्
को असमर्थ देखकर
पोप ने पेपीन
की सहायता माँगी
और उसने अपनी
फ्रैंक सेना से
लोंबार्द जाति
को हराकर
इटली का मध्य भाग
पोप के अधिकार
में दे दिया। उस
दिन से काथोलिक
चर्च का राज्य
विधिवत् प्रारंभ
हुआ और १८७० ई.
तक बना रहा।
(इ) पूर्व मध्यकाल
(७५०-१०५०)-
- पेपीन
के पुत्र चार्लमेन
(Charlemagne)
ने अपने दीर्घ
राज्यकाल (७६८-८१४ ई.)
में यूरोप की
राजनीतिक,
धार्मिक तथा सांस्कृतिक
एकता के लिये
सफल प्रयास किया।
उन्होंने स्पेन में
इस्लाम का विरोध
किया तथा उत्तर
में सैक्सन (Saxon)
जातियों को
हराकर उनको
ईसाई बनने
के लिये बाध्य
किया। उनके जीवनकाल
में सर्वत्र शिक्षा
का प्रचार तथा
धार्मिक उन्नति हुई।
किंतु उनकी मृत्यु
के बाद उनके साम्राज्य
का विघटन हुआ
और समस्त यूरोप
में अशांति फैल
गई। इसका कुप्रभाव
चर्च के संगठन
पर भी पड़ा। उस
युग को पश्चिम
के अध्यात्मिक पतन
का युग कहा गया
है। साधारण
पुरोहितों
में अनुशासनहीनता
बढ़ गई और
उसमें से बहुतों
ने विवाह किया
यद्यपि पाँचवीं
शताब्दी से पुरोहितों
के अविवाहित
रहने का नियम
चला आ रहा था।
बिशप तथा मठाध्यक्ष
सामंत भी थे
और उनके चुनाव
में बहुधा घूसखोरी
का हाथ रहा
करता था। पोप
अब राजा भी थे
तथा पेपल स्टेट्स
के शासन के लिये
बहुत से पुरोहित
राजनीतिक
मात्र ही रह गए
थे। पोपों के
चुनाव में रोमन
सामंतों की
प्रतियोगिता
भी होने लगी
तथा राजनीतिक
प्रतिद्वंद्वियों
द्वारा बहुत
से पोपों की
हत्या भी कर दी
गई थी। इस कारण
८८६ ई. से १०४३ ई. तक
३७ पोप हो गए।
उस पतन
के प्रतिक्रियास्वरूप
१०वीं शताब्दी में
फ्रांस के क्लुनी
(Cluny)
मठ नेतृत्व में
पश्चिम यूरोप
में मठवासी जीवन
का अपूर्व पुनर्विकास
हुआ। सैकड़ों दूसरे
उपमठ क्लुनी के
मठाध्यक्ष का अनुशासन
स्वीकार करते
थे जिससे पोप
के बाद क्लुनी
का मठाध्यक्ष उस
समय ईसाई संसार
का सबसे महत्वपूर्ण
व्यक्ति बन गया
था।
- कुंस्तुंतुनिया
के नेतृत्व में
नवीं शताब्दी
में बालकन की
स्लाव (Slav)
जातियों का
धर्मपरिवर्तन
हुआ और उसके
बाद रूस में भी
ईसाई धर्म का
विशेष विस्तार
हुआ। ईसाई धर्म
का सबसे बड़ा
दुर्भाग्य यह है
कि यूनानी भाषा
बोलनेवाले
प्राच्य काथोलिकों
तथा लैटिन भाषा
बोलनेवाले
पाश्चात्य कॉथोलिकों
का अलगाव उस युग
में बढ़ने लगा।
उसके कई कारण
हैं। यूनानी संस्कृति
लैटिन संस्कृति
से कहीं अधिक परिष्कृत
थी। एक ओर प्राच्य
चर्च तथा बीजैंटाइन
(Byzantine)
साम्राज्य का एकीकरण
हुआ था और
दूसरी ओर
पश्चिम में रहनेवाले
पोप को वहाँ
के शासकों से
सहायता मिला
करती थी। राजधानी
कुंस्तुंतुनिया
के बिशप को
पेत्रिआर्क की
उपाधि मिली थी
और उनका महत्व
इतना बढ़ गया
कि वह समस्त प्राच्य
चर्च के अध्यक्ष माने
जाते थे। इन सब
कारणों से पूर्व
में रोम के पोप
के अधिकार की
उपेक्षा होने
लगी। नवीं शताब्दी
में फोतियस
(Photius)
ने कुछ समय तक
प्राच्य चर्चों को
रोम से अलगकर
दिया था और
अपनी रचनाओं
में रोम के विरुद्ध
इतना कटु प्रचार
किया था कि, यद्यपि
उसने बाद में रोम
का अधिकार पुन:
स्वीकार कर
लिया, फिर भी
उसकी रचनाओं
का कुप्रभाव नहीं
मिट सका और
बाद में पेत्रिआर्क
माइकल सेरुलारियस
के समय में कुंस्तुंतुनिया
का चर्च रोम
से अलग हो गया
(१०५४ ई.)। इस्लाम ने काथॉलिक
चर्च को यूरोप
तक सीमित कर
दिया था, अब वह
पश्चिम यूरोप
तक ही सीमित
रहा।
(ई) उत्तर मध्यकाल
(१०५०-१५००)-
- ११वीं तथा १२वीं शताब्दियों
में चर्च ने बिशपों
की नियुक्ति तथा
पोप के चुनाव
में राजाओं
के हस्तक्षेप का
तीव्र विरोध
किया। पोप संत
लेओं नवम ने
(१०४१-१०५४) चर्च के अनुशासन
में बहुत सुधार
किया। १०५९ ई. में एक
कानून घोषित
किया गया कि
भविष्य में कार्डिनल
मात्र पोप का
चुनाव करेंगे;
बिशपों की नियुक्ति
के विषय में जर्मन
सम्राट् हेनरी
चतुर्थ और
पोप संत ग्रेगोरी
सप्तम में जो संघर्ष
हुआ, उसमें सम्राट्
को झुकना पड़ा
(१०७७ ई.)। अगली शताब्दी
में जर्मन सम्राट्
तथा कॉथोलिक
चर्च में समझौता
हुआ। बोर्म्स की
धर्मसंधि (११२३) के
अनुसार बिशपों
तथा मठाधीशों
की नियुक्ति में
शासकों का हस्तक्षेप
रुक गया। उस समय
से रोमन काथोलिक
चर्च का संगठन
रोम में केंद्रीभूत
हुआ। रोम के
प्रतिनिधि स्थायी
रूप से सभी देशों
में रहने लगे
तथा चर्च का
एक नया कानून
संग्रह सर्वत्र लागू
होने लगा।
११वीं शताब्दी
के उत्तरार्ध्
में उत्तर स्पेन के
इस्लाम विरोधी
अभियान को पर्याप्त
सफलता मिली
और ईसाई
सेनाओं ने १०८५ ई.
में तोलेदो
(Toledo)
को मुक्त किया।
पूर्व में १०७१ ई. में
बीजैंटाइन सम्राट्
की हार हुई।
इससे चिंतित हाकर
पोप ने ईसाई
राजाओं से
निवेदन किया
कि वे एशिया माइनर
तथा फिलिस्तीन
को इस्लाम से
मुक्त कर दें। फलस्वरूप
प्रथम क्रूसयुद्ध
(क्रूसेड) का आयोजन
किया गया (दे.
क्रूस युद्ध)। १०९९ ई.
में येरूसलेम
पर ईसाई सेनाओं
का अधिकार हुआ,
जो अधिक समय
तक नहीं रह सका।
- १२वीं श्ताब्दी
को पाश्चात्य चर्च
का उत्थान काल
माना जा सकता
है। पेरिस के
पीटर लोंबार्ड
की रचना से
धर्मविज्ञान (Theology)
को नया उत्साह
मिला तथा स्पेन
के पुरोहितों
ने अरबी भाषा
से अरस्तू के ग्रंथों
तथा उसको अरबी
व्यख्याओं का लैटिन
भाषा में अनुवाद
किया, जिससे
सर्वत्र दर्शनशास्त्र
में अभिरुचि जाग्रत
होने लगी।
उस शताब्दी
में अनेक नए धर्मसंघों
की उत्पत्ति हुई
जिनमें से दो
अत्यंत महत्वपूर्ण
हैं। सीतौ (Citeaux)
के धर्मसंघ की
स्थापना १०९८ ई. में
हुई थी। उस सिस्तर्सियन
(Cistercian)
संघ के मठ पश्चिम
यूरोप के जंगलों
में सर्वंत्र कृषि
का प्रचार करने
लगे। १२वीं शताब्दी
के अंत तक इस प्रकार
के ५३० मठों की स्थापना
हो चुकी थ। संत
बर्नाडं उस संघ
के सदस्य थे, उनकी
रचनाओं के
द्वारा ईसा और
उनकी माता मरिया
के प्रति कोमल
भक्ति का सर्वत्र
प्रचार हुआ।
संत नोर्बर्ट
(Norbert)
ने ११२० ई. में प्रेमोंस्त्राटेंशन
(Premonstratensian)
धर्मसंघ का प्रवर्तन
किया। उसके सदस्य
उपदेश दिया करते
थे तथा ईसाई
जनसाधारण
के लिय पुरोहितों
का कार्य भी करते
थे। वह संघ भी
शीघ्र ही फैल गया।
उस शताब्दी में
स्कैंडिनेविया,
मध्य जर्मनी, बोहेमिया,
प्रशा और पोलैंड
में जो धर्मप्रचार
का कार्य संपन्न
हुआ वह मुख्य रूप
से इन दो धर्मसंघों
के माध्यम से ही
संभव हो सका।
१२वीं शताब्दी के
उत्तरार्ध में सम्राट्
फ्रेड्रिक बरबारोस्सा
(११५२-११९०) ने फिर चर्च
पर अधिकार जताने
का प्रयास किया
किंतु पोप अलैक्जेंडर
तृतीय (११५९-११९१) ने उनका
सफलतापूर्वक
विरोध किया।
इसके अतिरिक्त
पोप अलेक्जैंडर
तृतीय ने चर्च
का संगठन भी
सुदृढ़ बनाया
जिससे वह दस
सर्वोत्तम पोपों
में गिने जाते
हैं।
- १३वीं शताब्दी के
प्रारंभ में दक्षिण
फ्रांस तथा उत्तर
इटली में प्रोवांस
के शासकों के
नेतृत्व में एलबीजेंसस
नामक संप्रदाय
के प्रचार से
जनता में अत्यधिक
अशांति फैल गई।
एलबीजेंसस भौतिक
जगत् तथा मानव
शरीर को दूषित
मानते थे इसलिये
संततिनिरोध
के उद्देश्य से विवाह
का विरोध तथा
उन्मुक्त प्रेम का समर्थन
करते थे। उस संप्रदाय
के उन्मूलन के लिये
एनक्विजिशन की
स्थापना हुई
थी (दे. एनक्विज़िशन)।
उस शताब्दी में
दो अत्यंत महत्वपूर्ण
धर्मसंघों की
स्थापना हुई
थी, फ्रांसिस्की
संघ तथा दोमिनिकी
संघ। इटली निवासी
संत फ्रांसिस
द्वारा स्थापित
धर्मसंघ में निर्धनता
पर विशेष बल
दिया जाता था।
प्रारंभ में उस
संघ के सदस्यों
में एक भी पुरोहित
नहीं था; फ्रांसिस्की
सन्यासी उपदेश
द्वारा जनता
में भक्ति तथा अन्य
धार्मिक भाव उत्पन्न
करते थे। इस संघ
को अपूर्व सफलता
मिली। १० वर्ष के
अंदर सदस्यों
की संख्या ५००० हो
गई थी और १२२१
ई. में उनकी प्रथम
सामान्य सभा
के अवसर पर
५०० नए उम्मेदवार
भरती होने
के लिये आए। संत
दोमिनिक स्पेनिश
थे। उन्होंने समझ
लिया कि एलबीजेंसस
का विरोध करने
के लिये ऐसे पुरोहितों
की आवश्यकता
है जो तपस्वी
हैं और विद्वान्
भी। अत: उन्होंने
अपने दोमिनिकी
संघ में तप तथा
विद्वत्ता पर विशेष
ध्यान दिया। यह
संघ फ्रांसिस्कों
संघ से कम लोकप्रिय
रहा, फिर भी
वह शीघ्र ही समस्त
यूरोप में फैल
गया।
यद्यपि पोप इन्नासेंट
तृतीय (११६८-१२१५) के समय
में ईसाई संसार
में पोप का प्रभाव
अपनी चरम सीमा
तक पहुँच गया
था, फिर भी १३वीं
शताब्दी में पोप
और जर्मन सम्राट
का संघर्ष होता
रहा। उदाहरणार्थ
१२४१ ई. में पोप के
मरते समय ११ कार्डिनल
जीवित थे; सम्राट्
ने दो को कैद
में डाल दिया,
दूसरे भाग
गए और दो वर्ष
तक चर्च का केई
परमाधिकारी
नहीं रहा। अंत
में फ्रांस के राजा
के अनुरोध से
सम्राट् ने चुनाव
होने दिया।
१३वीं शताब्दी में
यूरोप के विश्वविद्ययालयों
में कुछ समय तक
अरस्तू के अरबी
व्याख्याता अवेरोएस
(११२६-११९८ ई.) के मत तथा
स्कोलैस्टिक फिलोसोफी
का द्वद्वंयुद्ध हुआ,
जिसमें अंततोगत्वा
संत एलबेर्ट (११९३-१२८०),
संत बाना वेंच्यर
(१२२१-१२७४ ई.) तथा संत
थोमस अक्वाइनस
(१२२५-१२७४ ई.) के नेतृत्व
में स्कालैस्टिक
फिलोसोफी
की विजय हुई
और अरस्तू की
ईसाई व्याख्या
द्वारा ईसाई
धर्मसिद्धांतों
का युक्तिसंगत
प्रतिपादन हुआ।
उस समय समस्त यूरोप
में कला और
विशेषकर वास्तुकला
का विकास हुआ
और विशाल
भव्य गौदिक गिरजाघरों
का निर्माण प्रारंभ
हुआ।
- १३वीं शताब्दी
के अंत में पश्चिम
यूरोप में चर्च
का अपकर्ष प्रारंभ
हुआ और प्रोटेस्टैंट
विद्रोह तक उत्तरोत्तर
बढ़ता गया। उस
समय से जर्मन
सम्राट् के अतिरिक्त
फ्रांस के राजा
भी चर्च के मामलों
में अधिकाधिक
हस्तक्षेप करने
लगे। १३०५ ई. में एक
फ्रेंच पोप का
चुनाव हुआ, वह
जीवन भर फ्रांस
में ही रहे और
उनके फ्रेंच उत्तराधिकारी
भी १३६७ ई. तक अविज्ञोन
(Avignon)
नामक फ्रेंच नगर
में निवास करते
थे। उनमें से एक रोम
लौटे किंतु
वह एकाध वर्ष
बाद फिर फ्रांस
चले गए; उनके उत्तराधिकारी
ग्रेगोरी नवम
सिएना की संत
कैथरीन का
अनुरोध मानकर
१३७६ ई. में रोम
लौटे। उनकी मृत्यु
के बाद एक इटालियन
डर्बन षष्ठ को चुना
गया, क्योंकि जनता
ने कार्डिनलों
को धमकी दी
थी कि ऐसा न करने
पर उनकी हत्या
की जाएगी। डर्बन
के चुनाव के
बाद कार्डिनल
रोम से भाग
गए और उन्होंने
चार महीने
बाद एक नए पोप
को चुन लिया
जो अविज्ञोन
में निवास करने
लगे। अब पश्चिम
यूरोप में दो
पोप थे, एक राम
में और एक अविज्ञोन
में जिससे समस्त
काथलिक संसर
४० वर्ष तक दो
भागों में विभक्त
रहा। उस समस्या
का हल करने
के प्रयास में १४०९
ई. में एक तीसरे
पोप का भी चुनाव
हुआ किंतु १४१७ ई.
में सबों ने नवनिर्वाचित
मारतीन पंचम
को सच्चे पोप
के रूप में स्वीकार
किया और इस
तरह पाश्चात्य
विच्छेद (Western
schism) का अंत
हुआ।
इतने में
अंग्रेज वोक्लिफ
(Wycliffe)
सिखलाने लगा
कि चर्च का संगठन
(पोप, पुरोहित),
उसके संस्कार
आदि यह सब मनुष्य
का आविष्कार
है, ईसाइयों
के लिय बाइबिल
ही पर्याप्त है।
यह मत बोहेमिया
तक फैल गया
जहाँ जॉन हुस
(Hus)
उसका प्रचारक
और शहीद भी
बन गया (१४१५ ई.)। लूथर
पर उन सिद्धांतों
का प्रभाव स्पष्ट
है।
चर्च के अपकर्ष
का मुख्य कारण
१५वीं शताब्दी उत्तरार्ध
के नितांत अयोग्य
पोप ही हैं। यूरोप
में उस समय सर्वत्र
प्राचीन यूनानी
तथा लैटिन साहित्य
की अपूर्व लोकप्रियता
के साथ साथ एक
नवीन सांस्कृतिक
आंदोलन प्रांरभ
हुआ जिसे रिनेसाँ
अथवा नवजागरण
कहा गया है। बीजैंटाइन
साम्राज्य का अंत
निकट देखकर
बहुत से यूनानी
विद्वान् पश्चिम
में आकर बसने
लगे। उनकी संख्या
और बढ़ गई
जब १४५३ ई. में कुस्तुंतुनिया
इस्लाम के अधिकार
में आया। उन यूनानी
विद्वानों से
नवजागरण आंदोलन
को और प्रोत्साहन
मिला। रोम
के पोप उस आंदोलन
के संरक्षक बन
गए और उन्होंने
रोम को नवजागरण
का एक मुख्य केंद्र
बना लिया। नैतिकता
और धर्म की
उपेक्षा होने
लगी और १५वीं
शताब्दी के अंत
तक रोम का
दरबार व्यभिचारव्याप्त
रहा। इसके अतिरिक्त
पोपों के चुनाव
में राजनीति
के हस्तक्षेप तथा
इटली के अभिजात
वर्ग की प्रतियोगिता
ने भी रोम के
प्रति ईसाई संसार
की श्रद्धा को बहुत
ही घटा दिया।
असंतोष का एक
और कारण यह
था कि समस्त चर्च
की संस्थाओं पर
उनकी संपत्ति के
अनुसार कर लगाया
जाता था और
रोम के प्रतिनिधि
सर्वत्र घूमकर
यह रुपया वसूल
करते थे।
(उ) आधुनिक काल
(१५०० ई. से)-
- लूथर ने १५१७ ई.
में काथलिक चर्च
की बुराइयों
के विरुद्ध आवज
उठाई किंतु वह
शीघ्र ही कुछ परंपरागत
ईसाई धर्मसिद्धांतों
का भी विरोध
करने लगा। इस
प्रकार एक नए संप्रदाय
की उत्पत्ति हुई
(दे. लूथर)। लूथर
को जर्मन शासकों
का संरक्षण मिला
और जर्मनी
के अतिरिक्त स्कैंडिनेविया
के समस्त ईसाई
उनके संप्रदाय
में सम्मिलित हुए।
बाद में कालविन
ने लूथर के
सिद्धांतों का
विकसित करते
हुए एक दूसरे
प्रोटेस्टैंट संप्रदाय
का प्रवर्तन किया
जो स्विट्जरलैंड,
स्काटलैंड, हालैंड
तथा फ्रांस के
कुछ भागों में
फैल गया (दे.
प्रेस्बिटरीय
धर्म)। अंत में हेनरी
अष्टम ने भी इंग्लैड
को रोम के
अधिकार से अलग
कर दिया जिससे
ऐंग्लिकन चर्च प्रारंभ
हुआ (दे. ऐंग्लिकन
समुदाय)।
- प्रोटेस्टैंट
विद्रोह के प्रतिक्रिया
स्वरूप कैथलिक
चर्च में 'काउंटर
रिफॉर्मेशन'
(प्रतिसुधारांदोलन)
का प्रवर्तन हुआ।
१६वीं शताब्दी के
महान् पोपों
के नेतृत्व में
चर्च के शासन
में अध्यात्म को फिर
प्राथमिकता मिल
गई; बहुत से
नए धर्मसंघों
की स्थापना हुई
जिसमें थिआटाइन
तथा जेसुइट प्रमुख
हैं (दे. जेसुइट)।
प्राची धर्मसंघों
में, विशेषकर
फ्रांसिस्की तथा
कार्मेलाइट धर्मसंघ
में सुधार लाया
गया; बहुत से
संत उत्पन्न हुए जिनमें
संत तेरेसा
(१५१५-१५८२ ई.) तथा संत
जॉन ऑव दि क्तोस
(१५४२-१५९१) अपनी रहस्यवादी
रचनाओं के
कारण अमर हो
गए हैं। धर्मप्रचार
(मिशन) का कार्य
नवीन उत्साह से
अमरीका तथा
एशिया में फैलने
लगा (दे. धर्मप्रचार)।
ट्रेंट (Trent)
में चर्च की १९वीं
विश्वसभा का आयोजन
किया गया किंतु
प्रोटेस्टैंटों
ने इसमें भाग
लेने से इनकार
कर दिया। इस
विश्वसभा को
कई बार स्थगित
कर दिया गया
जिससे वह १५४५ ई.
में प्रारंभ होकर
केवल १५६३ ई. में समाप्त
हो गई। पुराहितों
के शिक्षण तथा
चर्च के संगठन
के नए नियमों
के अतिरिक्त प्रोटेस्टैंट
संप्रदाय के विरोध
में परंपरागत
कॉथलिक धर्मसिद्धांतों
का सूत्रीकरण
भी हुआ। उस समय
से पश्चिम यूरोप
के ईसाई संसार
में एकता लाने
की आशा बहुत
क्षीण हो गई।
परवर्ती शताब्दियों
में समस्त पश्चिम
यूरोप में नास्तिकता
तथा अविश्वास व्यापक
रूप से फैल गया।
फ्रेंच क्रांति के
फलस्वरूप चर्च
की अधिकांश जायदाद
जब्त हुई और
चर्च तथा सरकार
का गहरा संबंध
सर्वदा के लिये
टूट गया। १८७० ई.
में इटालियन
क्रांति ने पेपल
स्टेट्स पर भी
अधिकार कर लिया,
इस कारण जो
समस्या उत्पनन हुई
वह १९२९ ई. में हल
हो गई (दे. वैटिकन)।
- २०वीं शताब्दी के
प्रारंभ में ईसाई
एकता का आंदोलन
(एकूमेनिकल मूवमेंट)
प्रारंभ हुआ।
उस समय तक प्रोटेस्टैंट
धर्म बहुत से
संप्रदायें में
विभक्त हो गया
था और इस कारण
धर्मप्रचार के
कर्य में कठिनाई
का अनुभव हुआ।
१९१० में एडिनबर्ग में
प्रथम वर्ल्ड मिशनरी
कॉनफरेंस
का अधिवेशन हुआ।
इस आंदोलन
के फलस्वरूप वर्ल्ड
कौंसिल ऑव
चर्चेंज का संगठन
हुआ जिसका पिछला
अधिवेशन १९६१ ई. में
दिल्ली में हुआ
है। सभी मुख्य प्रोटेस्टैंट
संप्रदाय तथा
प्राच्य ओर्थोदोक्स
चर्च उस संस्था
के सदस्य हैं और
र्कांथलिक ऑबजर्वर
(पर्यवेक्षक) उसकी
सभाओं में उपस्थित
रहते हैं। उसी
प्रकार १९६२ ई. में
रोम में कॉथलिक
चर्च की जो २१वीं
विश्वसभा प्रारंभ
हुई उसके लिये
मुख्य प्रोटेंस्टैंट
संप्रदायों ने
तथा प्राच्य आथदोक्स
चर्च ने अपने लिये
मुख्य प्रोटेस्टैंट
संप्रदायों ने
तथा प्राच्य आथदोक्स
चर्च ने अपने प्रतिनिधि
भेजे। इस प्रकार
हम देखते हैं
कि ईसाई संसार
में एकता का आंदोलन
आशातीत प्रगति
से आगे बढ़ता
जा रहा है।
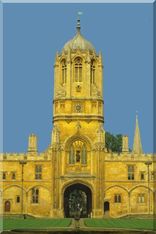 चर्च
यह शब्द यूनानी
विशेषण का अपभ्रंश
है जिसका शाब्दिक
अर्थ है 'प्रभु का'।
वास्तव में चर्च
(और गिरजा
भी) दो अर्थों में
प्रयुक्त है; एक तो
प्रभु का भवन अर्थात्
गिरजाघर तथा
दूसरा, ईसाइयों
का संगठन। चर्च
के अतिरिक्त कलीसिया
शब्द भी चलता है।
यह यूनानी बाइबिल
के एक्लेसिया शब्द
काविकृत रूप
है; बाइबिल में
इसका अर्थ है किसी
स्थानविशेष अथवा
विश्व भर के ईसाइयों
का समुदाय। बाद
में यह शब्द गिरजाघर
के लिये भी प्रयुक्त
होने लगा। यहाँ
पर संस्था के अर्थ
में चर्च पर विचार
किया जायगा।
दूसरे अर्थ के
लिये दे. ''गिरजाघर।''
चर्च
यह शब्द यूनानी
विशेषण का अपभ्रंश
है जिसका शाब्दिक
अर्थ है 'प्रभु का'।
वास्तव में चर्च
(और गिरजा
भी) दो अर्थों में
प्रयुक्त है; एक तो
प्रभु का भवन अर्थात्
गिरजाघर तथा
दूसरा, ईसाइयों
का संगठन। चर्च
के अतिरिक्त कलीसिया
शब्द भी चलता है।
यह यूनानी बाइबिल
के एक्लेसिया शब्द
काविकृत रूप
है; बाइबिल में
इसका अर्थ है किसी
स्थानविशेष अथवा
विश्व भर के ईसाइयों
का समुदाय। बाद
में यह शब्द गिरजाघर
के लिये भी प्रयुक्त
होने लगा। यहाँ
पर संस्था के अर्थ
में चर्च पर विचार
किया जायगा।
दूसरे अर्थ के
लिये दे. ''गिरजाघर।''