 कृंतक
(Rodentia) वर्तमान
स्तनधारियों
में सर्वाधिक
सफल एवं समृद्ध
गण कृंतकों
का है, जिसमें
१०१ जातियाँ जीवित
प्राण्योिं की तथा
६१ जातियाँ अश्मीभूत
(Fossilized) प्राणियों
की रखी गई हैं।
जहाँ तक जातियों
का प्रश्न है, समस्त
स्तनधारियों
के वर्ग में लगभग
४,५०० जातियों के
प्राणी आजकल जीवित
पाए जाते हैं, जिनमें
से आधे से भी अधिक
(२,५०० के लगभग) जातियों
के प्राणी कृंतकगण
में ही आ जाते
हैं। शेष २,००० जातियों
के प्राणी अन्य २० गणों
में आते हैं। इस गण
में गिलहरियाँ,
हिममूष, (Marmots)
उड़नेवाली
गिलहरियाँ
(Flyiug squirrels)
श्वमूष,
(Prairie dogs) छछूँदर
(Musk rats) ,
धानीमूष, (Pocket
dogs) ऊ द (Beavers),
चूहे (Rats),
मूषक (Mice)
, शाद्वलमूषक
(Voles),
जवितमूष (Gerbille)
, वेणमूषक
(Bamboo rats),
साही (Porcupines)
, बंटमूष
(Guinea pigs),
आदि स्तनधारी
प्राणी आते हैं।
कृंतक
(Rodentia) वर्तमान
स्तनधारियों
में सर्वाधिक
सफल एवं समृद्ध
गण कृंतकों
का है, जिसमें
१०१ जातियाँ जीवित
प्राण्योिं की तथा
६१ जातियाँ अश्मीभूत
(Fossilized) प्राणियों
की रखी गई हैं।
जहाँ तक जातियों
का प्रश्न है, समस्त
स्तनधारियों
के वर्ग में लगभग
४,५०० जातियों के
प्राणी आजकल जीवित
पाए जाते हैं, जिनमें
से आधे से भी अधिक
(२,५०० के लगभग) जातियों
के प्राणी कृंतकगण
में ही आ जाते
हैं। शेष २,००० जातियों
के प्राणी अन्य २० गणों
में आते हैं। इस गण
में गिलहरियाँ,
हिममूष, (Marmots)
उड़नेवाली
गिलहरियाँ
(Flyiug squirrels)
श्वमूष,
(Prairie dogs) छछूँदर
(Musk rats) ,
धानीमूष, (Pocket
dogs) ऊ द (Beavers),
चूहे (Rats),
मूषक (Mice)
, शाद्वलमूषक
(Voles),
जवितमूष (Gerbille)
, वेणमूषक
(Bamboo rats),
साही (Porcupines)
, बंटमूष
(Guinea pigs),
आदि स्तनधारी
प्राणी आते हैं।
पृथ्वी
पर जहाँ भी प्राणियों का आवास संभव है वहाँ कृंतक अवश्य पाए जाते हैं। ये
हिमालय पर्वत पर २०,००० फुट की ऊँचाई तक और नीचे समुद्र तल तक पाए जाते
हैं। विस्तार में ये उष्णकटिबंध से लेकर लगभग ध्रुवप्रदेशों तक मिलते हैं।
ये मरु स्थल उष्णप्रधान वर्षावन, दलदल और मीठे जलाशय-सभी
स्थानों पर मिलते हैं: कोई समुद्री कृंतक अभी तक देखने में नहीं आया है।
अधिकांश कृंतक स्थलचर हैं और प्राय: बिलों में रहते हैं, किंतु कुछेक जैसे
गिलहरियाँ आदि, वृक्षाश्रयी हैं। कुछ कृंतक उड़ने का प्रयत्न भी कर रहे हैं,
फलत: उड़नेवाली गिलहरियों का विकास हो चुका है। इसी प्रकार, यद्यपि अभी तक
पूर्ण रूप से जलाश्रयी कृंतकों का विकास नहीं हो सका है, फिर भी ऊद तथा
छछूँदर इस दिशा में पर्याप्त आगे बढ़ चुके हैं।
लाक्षणिक विशेषताएँ-कृंतकों की प्रमुख लाक्षणिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- इनमें श्वदंतों (Canines) तथा अगले प्रचर्वण दंतों की अनुपस्थिति के कारण दंतावकाश (Diastema) पर्याप्त विस्तृत होता है।
-
केवल चार कर्तनक दंत (Incisors) होते है-दो ऊपर वाले जबड़े में और दो नीचेवाले जबड़े में। दाँत लंबे तथा पुष्ट होते हैं और आजीवन बराबर बढ़ते रहते हैं। इनमें इनैमल (Enamel) मुख्य
रूप से अगले सीमांत पर ही सीमित रहता है, जिससे ये घिसकर छेनी सरीखे हो
जाते हैं और व्यवहार में आते रहने के कारण आप ही आप तीक्ष्ण भी होते रहते
हैं। कुतरने के लिए इस रीति के विकास के अतिरिक्त कृंतक स्तनधारी ही कहे जा
सकते हैं।
- अधिकांश स्तनधारी अपना
भोजन मनुष्य के समान चबाते हैं। चबाते समय निचला जबड़ा मुख्य रूप से ऊपर की
दिशा में ही गति करता है। कृंतकों में इसके विपरीत चर्वण की क्रिया निचले
जबड़े की आगे पीछे की दिशा में होनेवाली गति के परिणामस्वरूप होती है। इस
प्रकार की गति के लिए हनुपेशियाँ बलशाली तथा जटिल होती है।
- अन्य शाकाहारी प्राणियों के सदृश कृंतकों के आहारमार्ग में सीकम (Caecum) बहुत
बड़ा होता है, परंतु अमाशय का विभाजन केवल मूषकों में ही देखने को मिलता
है। इसमें हृदय की ओर वाले भाग में श्रैंगिक आस्तर चढ़ा होता है।
-
मस्तिष्कपिंड चिकना होता है, जिसमें खाँचे (Furrows) बहुत कम होते हैं। फलत: इनकी मेधाशक्ति अधिक नहीं होती।
- वृषण साधारणतया उदरस्थ होते हैं।
- गर्भाशय प्राय: दोहरा होता है।
- देखने में प्लासेंटा (Placenta) विविधरूपी होता हैं, किंतु प्राय: बिंबाभी (discoidal) तथा शोणगर्भवेष्टित (haemochorial) ढंग का होता है।
- कुछ कृंतकों की गर्भाविधि केवल १२ दिन की होती है।
- कुहनी संधि (Elbowjoint) चारों ओर घूम सकती है।
-
चारों हाथ पैर नखरयुक्त (clawed) होते
हैं तथा चलते समय पूरा पदतल भूमि पर पड़ता है। अगले पैर (हाथ) प्राय: पिछले
पैरों की अपेक्षा छोटे होते हैं और भोजन को उठाकर खाने में सहायक होते
हैं। कभी-कभी यह प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ी हुई होती है कि ये दो ही (पिछले)
पैरों से कूदते हुए चलते हैं।
वर्गीकरण-कृतंकों
के वर्गीकरण में मुख्य आधार हनुपेशियों की विभिन्नता तथा इनके संबद्ध कपाल
की सरंचनाओं को ही माना गया है। इस प्रकार कृंतक गण को तीन उपगणों में विभाजित किया गया है:
-
साइयूरोमॉर्फ़ा (Sciuromorpha) अर्थात गिलहरी सदृश कृतक,
-
माइयोमॉर्फ़ा (Myomorpha) अर्थात, मूषकों जैसे कृंतक तथा
-
हिस्ट्रिकोमॉर्फ़ा (Hystricomorpha) अर्थात् साही के अनुरूप कृंतक।
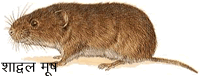 साइयूरोमॉर्फ़ा-इस
उपगण की लाक्षणिक
विशेषताएँ ये
हैं : एक तो इनके
ऊपरी जबड़े में
दो चवर्णदंत
(Masseter) होते
हैं तथा निचले
जबड़े में केवल
एक, और दूसरे
एक चर्वणपेशी
(Infra-orbital canal)
होती
है, जो अक्ष्यध:कुल्या
से होकर नहीं
जाती। कृंतकों
के इस आद्यतम उपगण
में गिलहरियों,
उड़नेवाली गिलहरियों
तथा ऊदों के अतिरिक्त
सिवेलेल (Sewellel)
जैसे बहुत
ही पुरातन कृंतक
तथा पुरानूतन
(Plaeocene) युग
के प्राचीनतम
अश्मीभूत कृंतक
भी रखे जाते
हैं। यही नहीं, इस
उपगण में कृंतकों
के कुछ ऐसे वंश
भी आते हैं जिनके
संबंधसादृश्य
अनिश्चित हैं।
साइयूरोमॉर्फ़ा-इस
उपगण की लाक्षणिक
विशेषताएँ ये
हैं : एक तो इनके
ऊपरी जबड़े में
दो चवर्णदंत
(Masseter) होते
हैं तथा निचले
जबड़े में केवल
एक, और दूसरे
एक चर्वणपेशी
(Infra-orbital canal)
होती
है, जो अक्ष्यध:कुल्या
से होकर नहीं
जाती। कृंतकों
के इस आद्यतम उपगण
में गिलहरियों,
उड़नेवाली गिलहरियों
तथा ऊदों के अतिरिक्त
सिवेलेल (Sewellel)
जैसे बहुत
ही पुरातन कृंतक
तथा पुरानूतन
(Plaeocene) युग
के प्राचीनतम
अश्मीभूत कृंतक
भी रखे जाते
हैं। यही नहीं, इस
उपगण में कृंतकों
के कुछ ऐसे वंश
भी आते हैं जिनके
संबंधसादृश्य
अनिश्चित हैं।
साइयूरोमॉर्फ़ा में कृंतकों के १३ कुल रखे गए हैं। इस्काइरोमाइडी (Ischyromyidae) नामक कुल में रखे गए सभी प्राणी यूरेशिया तथा उत्तरी अमरीका के पुरानूतन से लेकर मध्यनूतम (Miocene) युगों तक के प्रस्तरस्तरों में पाए जाते हैं। इस वंश का एक उदाहरण पैरामिस (Paramys) है, जो पुरानूतन से प्रादिनूतन (Eocene) युगों तक के प्रस्तरस्तरों में पाया गया है। साइयूरोमॉर्फ़ा कृंतकों का दूसरा महत्वपूर्ण वंश ऐप्लोडौंटाइडी (Aplodontidae) है, जिसका उदाहरण ऐप्लोडौंशिया (Aplodontia) ,
या सीवलेल, उत्तरी अमरीका के उत्तर पश्चिमी भागों में पाया जानेवाला एक
बहुत ही पुरातन कृंतक है। यह लगभग १२ इंच लंबा, स्थूल आकार का तथा छोटी
दुमवाला प्राणी होता है, जो किसी सीमा तक जलचर भी कहा जा सकता है।
 तीसरा
महत्वपूर्ण कुल
साइयूरिडी (Sciuridae)
हैं, जिसमें
वृक्षचारी गिलहरियाँ
(Ratufa),
उड़न गिलहरियाँ,
(Prtaurista) , स्थलचारी
गिलहरियाँ
(Citellus),
हिममूष (Marmoda),
चिपमंक (Tamias,
Eutamias) आदि
कृंतक आते हैं।
उपर्युक्त दोनों
कुलों के प्राणियों
से गिलहरियाँ
कुछ अधिक विकसित
कृंतक हैं। ये
आस्ट्रेलिया के
अतिरिक्त अन्य सभी
महाद्वीपों में
पाई जाती हैं।
भारत की सबसे
साधारण पंचरेखिनी
गिलहरी (Funambulus
Pennanti) है, जिसके
गहरे भूरे शरीर
पर लंबाई की
दिशा में आगे
से पीछे तक जाती
है अपेक्षाकृत
हल्के रंग की पाँच
धारियाँ होती
है। यह मुख्य रूप
से उत्तरी भारत
में मनुष्य के निवासस्थानों
के आस-पास मिलती
हैं, इन्हें पाल भी
सकते हैं। दूसरी
साधारण गिलहरी
मुख्य रूप से दक्षिण
भारत में पाई
जानेवाली त्रिरेखिनी
है, जिसकी पीठ
पर केवल तीन
धारियाँ होती
हैं। ये जंगलों
में ही रहती हैं
और पकड़कर पालतू
बनाने का प्रयत्न
किए जाने पर कुछ
ही सप्ताहों में
मर जाती हैं।
गिलहरियों
की संबंधी आकंदलिकाएँ,
या उड़न गिलहरियाँ,
मुख्यत: वनचोरी
होती हैं। गरदन
के पीछे से लेकर
पिछली टाँगों
के अगले भाग तक
जाती हुई चर्मावतारिका
(Patagium) नामक
एक लोचदार झिल्ली
सरीखी रचना,
जो इनके सारे
धड़ से चिपकी रहती
है, इन प्राणियों
को ऊँचे-ऊँचे
पेड़ों से नीचे
भूमि पर, अथवा
निचली शाखाओं
पर, उतरने में
सहायता पहुँचाती
है। उड़न गिलहरियों
की इस गति को
हम उड़ान तो नहीं
कह सकते, विसर्पण
(gliding) अवश्य
कह सकते हैं। ये
प्राणी मुख्यत: एशिया
के उष्णप्रधान भागों
में पाए जाते हैं।
यद्यपि यूरोप
तथा उत्तरी अमरीका
में भी इनके प्रतिनिधियों
का अभाव नहीं है।
तीसरा
महत्वपूर्ण कुल
साइयूरिडी (Sciuridae)
हैं, जिसमें
वृक्षचारी गिलहरियाँ
(Ratufa),
उड़न गिलहरियाँ,
(Prtaurista) , स्थलचारी
गिलहरियाँ
(Citellus),
हिममूष (Marmoda),
चिपमंक (Tamias,
Eutamias) आदि
कृंतक आते हैं।
उपर्युक्त दोनों
कुलों के प्राणियों
से गिलहरियाँ
कुछ अधिक विकसित
कृंतक हैं। ये
आस्ट्रेलिया के
अतिरिक्त अन्य सभी
महाद्वीपों में
पाई जाती हैं।
भारत की सबसे
साधारण पंचरेखिनी
गिलहरी (Funambulus
Pennanti) है, जिसके
गहरे भूरे शरीर
पर लंबाई की
दिशा में आगे
से पीछे तक जाती
है अपेक्षाकृत
हल्के रंग की पाँच
धारियाँ होती
है। यह मुख्य रूप
से उत्तरी भारत
में मनुष्य के निवासस्थानों
के आस-पास मिलती
हैं, इन्हें पाल भी
सकते हैं। दूसरी
साधारण गिलहरी
मुख्य रूप से दक्षिण
भारत में पाई
जानेवाली त्रिरेखिनी
है, जिसकी पीठ
पर केवल तीन
धारियाँ होती
हैं। ये जंगलों
में ही रहती हैं
और पकड़कर पालतू
बनाने का प्रयत्न
किए जाने पर कुछ
ही सप्ताहों में
मर जाती हैं।
गिलहरियों
की संबंधी आकंदलिकाएँ,
या उड़न गिलहरियाँ,
मुख्यत: वनचोरी
होती हैं। गरदन
के पीछे से लेकर
पिछली टाँगों
के अगले भाग तक
जाती हुई चर्मावतारिका
(Patagium) नामक
एक लोचदार झिल्ली
सरीखी रचना,
जो इनके सारे
धड़ से चिपकी रहती
है, इन प्राणियों
को ऊँचे-ऊँचे
पेड़ों से नीचे
भूमि पर, अथवा
निचली शाखाओं
पर, उतरने में
सहायता पहुँचाती
है। उड़न गिलहरियों
की इस गति को
हम उड़ान तो नहीं
कह सकते, विसर्पण
(gliding) अवश्य
कह सकते हैं। ये
प्राणी मुख्यत: एशिया
के उष्णप्रधान भागों
में पाए जाते हैं।
यद्यपि यूरोप
तथा उत्तरी अमरीका
में भी इनके प्रतिनिधियों
का अभाव नहीं है।
इस उपगण का चौथा महत्वपूर्ण वंश कैस्टॉरिडी (Castoridae) है, जिसके प्रतिनिधि ऊद अपने परिश्रम तथा जलचर प्रकृति के लिए प्रसिद्ध हैं। किसी समय ये विश्व के सारे उत्तरध्रुवीय भूभाग (North Arctic regions) में पाए जाते थे और जंगली प्रदेशों में रहते थे। इनका समूर (fur) बहुत
मूल्यवान माना जाता है, जिसके कारण इनका भयंकर संहार हुआ और ये लुप्तप्राय
कर दिए गए। ये बड़े कुशल वनवासी कहे जा सकते हैं, क्योंकि किस पेड़ की किस
प्रकार काटा जाए कि वह एक निश्चित दिशा में गिरे, यह ये भली-भाँति जानते
हैं। पेड़ों को जल में गिराकर ये बाँध बाँधते हैं। इस प्रकार एक तालाब सा
बनाकर उसमें कीचड़ और टहनियों की सहायता से अपने घर बनाते हैं। पेड़ों की छाल
खाने के काम में लाते हैं। कृंतकों में किसी अन्य प्राणी की शरीर रचना
जलचारी जीवन के लिए इतनी अधिक रूपांतरित नहीं होती जितनी ऊद की। यही नहीं,
दक्षिण अमरीका के कुछ प्राणियों के अतिरिक्त ऊद सबसे अधिक बड़े कृंतक होते
हैं। प्रातिनूतन (Pleistocene) युग
में तो यूरोप तथा उत्तरी अमरीका दोनों ही दिशा में और भी अधिक बड़े-बड़े ऊद
पाए जाते थे, जो आकार में छोटे-मोटे भालू के बराबर होते थे। (देखें ऊद)।
मायोमॉर्फ़ा-इस
उपगण में परिगणित कृंतकों की चर्वणपेशी का मध्य भाग अक्ष्यध:कुल्या से
होकर जाता है। इस उपगण में कम से कम २०० जातियों तथा लगभग ७०० जातों के
कृंतक आते हैं। इस प्रकार आधुनिक स्तनियों में यह सबसे बड़ा प्राणिसमूह है।
यही नहीं, अनेक दृष्टियों से हम इस प्राणिसमूह को स्तनधारियों में सर्वाधिक
सफल भी पाते हैं। इस उपगण में आने वाले कृंतकों के उदाहरण हैं :
डाइपोडाइडी (Diepodidae) कुल के चपलाखु (Jerboas); क्राइसेटाइडी (Cricetidae) कुल के शाद्वल मूष (Voles), मृगाखु (Deer mouse) तथा संयाति (Lemmings); म्यूराइडी (Muridae) कुल के मूष (Rats) , मूषक (Mice), स्वमूषक (Dormice), क्षेत्रमूषिका (Field mice) आदि तथा ज़ेपाडाइडी (Zapodidae) कुल के प्लुतमूषक (Jumping mice)। इनके अतिरिक्त इस उपगण में पाँच कुल और भी हैं।
इन
प्राणियों ने अपने को लगभग सभी प्रकार के वातावरणों के अनुकूल बनाया है।
कुछ स्थलचारी हैं, कुछ उपस्थलचारी, कुछ वृक्षाश्रीय हैं, कुछ दौड़ में तेज
कूदते हुए चलते हैं, कुछ उड्डयी (Volant) होते हैं और कुछ जलचारी होते हैं।
हिस्ट्रिकोमॉफ़ी-यह
उपगण भी कृंतकों का काफ़ी बड़ा उपगण है, जिसमें १९ कुल रखे गए हैं। इन
कृंतकों में चर्वणपेशी के मध्य भाग को स्थान देने के लिए अक्ष्यध:कुल्या
पर्याप्त बड़ी होती है, परंतु उसका पार्श्व भाग गंडास्थि (Zygoma) से
जुड़ा होता है। एशिया तथा अफ्रीका के ऊद और उत्तरी अमरीका के कतिपय भिन्न
ऊदों के अतिरिक्त इस उपगण के शेष सभी कृंतक दक्षिणी अमरीका में ही सीमित
हैं। यही नहीं, इस उपगण के प्राणियों के जीवाश्म (fossils) भी दक्षिणी अमरीका के आदिनूतन (Oligocene) युग में ही मिले हैं। इस उपगण का प्रत्येक प्राणी वैज्ञानिकों के लिए बड़े महत्व का है।
मानव हित की दृष्टि से
कृंतक बड़े ही आर्थिक महत्व के हैं। जहाँ तक हानियों का संबंध है, ये खेती,
घर के सामान तथा अन्य वस्तुओं को अत्यधिक मात्रा में नष्ट किया करते हैं।
प्लेग फैलाने में चूहा कितना सहायक होता है, यह किसी से छिपा नहीं। जहाँ तक
लाभ का संबंध है, इनकी कई जातियाँ प्रयोगशाला में विभिन्न रोगों की रोकथाम
के लिए किए जानेवाले प्रयोगों में काम में लाई जाती हैं। कई जातियों का
लोमश चर्म और मांस उपयोगी होता है और कई जातियाँ हानिकर कीटों तथा कृमियों
का आहारकर उन्हें नष्ट किया करती हैं। (शै. मो. दा.)
 कृंतक
(Rodentia) वर्तमान
स्तनधारियों
में सर्वाधिक
सफल एवं समृद्ध
गण कृंतकों
का है, जिसमें
१०१ जातियाँ जीवित
प्राण्योिं की तथा
६१ जातियाँ अश्मीभूत
(Fossilized) प्राणियों
की रखी गई हैं।
जहाँ तक जातियों
का प्रश्न है, समस्त
स्तनधारियों
के वर्ग में लगभग
४,५०० जातियों के
प्राणी आजकल जीवित
पाए जाते हैं, जिनमें
से आधे से भी अधिक
(२,५०० के लगभग) जातियों
के प्राणी कृंतकगण
में ही आ जाते
हैं। शेष २,००० जातियों
के प्राणी अन्य २० गणों
में आते हैं। इस गण
में गिलहरियाँ,
हिममूष, (Marmots)
उड़नेवाली
गिलहरियाँ
(Flyiug squirrels)
श्वमूष,
(Prairie dogs) छछूँदर
(Musk rats) ,
धानीमूष, (Pocket
dogs) ऊ द (Beavers),
चूहे (Rats),
मूषक (Mice)
, शाद्वलमूषक
(Voles),
जवितमूष (Gerbille)
, वेणमूषक
(Bamboo rats),
साही (Porcupines)
, बंटमूष
(Guinea pigs),
आदि स्तनधारी
प्राणी आते हैं।
कृंतक
(Rodentia) वर्तमान
स्तनधारियों
में सर्वाधिक
सफल एवं समृद्ध
गण कृंतकों
का है, जिसमें
१०१ जातियाँ जीवित
प्राण्योिं की तथा
६१ जातियाँ अश्मीभूत
(Fossilized) प्राणियों
की रखी गई हैं।
जहाँ तक जातियों
का प्रश्न है, समस्त
स्तनधारियों
के वर्ग में लगभग
४,५०० जातियों के
प्राणी आजकल जीवित
पाए जाते हैं, जिनमें
से आधे से भी अधिक
(२,५०० के लगभग) जातियों
के प्राणी कृंतकगण
में ही आ जाते
हैं। शेष २,००० जातियों
के प्राणी अन्य २० गणों
में आते हैं। इस गण
में गिलहरियाँ,
हिममूष, (Marmots)
उड़नेवाली
गिलहरियाँ
(Flyiug squirrels)
श्वमूष,
(Prairie dogs) छछूँदर
(Musk rats) ,
धानीमूष, (Pocket
dogs) ऊ द (Beavers),
चूहे (Rats),
मूषक (Mice)
, शाद्वलमूषक
(Voles),
जवितमूष (Gerbille)
, वेणमूषक
(Bamboo rats),
साही (Porcupines)
, बंटमूष
(Guinea pigs),
आदि स्तनधारी
प्राणी आते हैं।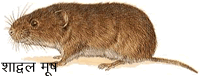 साइयूरोमॉर्फ़ा-इस
उपगण की लाक्षणिक
विशेषताएँ ये
हैं : एक तो इनके
ऊपरी जबड़े में
दो चवर्णदंत
(Masseter) होते
हैं तथा निचले
जबड़े में केवल
एक, और दूसरे
एक चर्वणपेशी
(Infra-orbital canal)
होती
है, जो अक्ष्यध:कुल्या
से होकर नहीं
जाती। कृंतकों
के इस आद्यतम उपगण
में गिलहरियों,
उड़नेवाली गिलहरियों
तथा ऊदों के अतिरिक्त
सिवेलेल (Sewellel)
जैसे बहुत
ही पुरातन कृंतक
तथा पुरानूतन
(Plaeocene) युग
के प्राचीनतम
अश्मीभूत कृंतक
भी रखे जाते
हैं। यही नहीं, इस
उपगण में कृंतकों
के कुछ ऐसे वंश
भी आते हैं जिनके
संबंधसादृश्य
अनिश्चित हैं।
साइयूरोमॉर्फ़ा-इस
उपगण की लाक्षणिक
विशेषताएँ ये
हैं : एक तो इनके
ऊपरी जबड़े में
दो चवर्णदंत
(Masseter) होते
हैं तथा निचले
जबड़े में केवल
एक, और दूसरे
एक चर्वणपेशी
(Infra-orbital canal)
होती
है, जो अक्ष्यध:कुल्या
से होकर नहीं
जाती। कृंतकों
के इस आद्यतम उपगण
में गिलहरियों,
उड़नेवाली गिलहरियों
तथा ऊदों के अतिरिक्त
सिवेलेल (Sewellel)
जैसे बहुत
ही पुरातन कृंतक
तथा पुरानूतन
(Plaeocene) युग
के प्राचीनतम
अश्मीभूत कृंतक
भी रखे जाते
हैं। यही नहीं, इस
उपगण में कृंतकों
के कुछ ऐसे वंश
भी आते हैं जिनके
संबंधसादृश्य
अनिश्चित हैं। तीसरा
महत्वपूर्ण कुल
साइयूरिडी (Sciuridae)
हैं, जिसमें
वृक्षचारी गिलहरियाँ
(Ratufa),
उड़न गिलहरियाँ,
(Prtaurista) , स्थलचारी
गिलहरियाँ
(Citellus),
हिममूष (Marmoda),
चिपमंक (Tamias,
Eutamias) आदि
कृंतक आते हैं।
उपर्युक्त दोनों
कुलों के प्राणियों
से गिलहरियाँ
कुछ अधिक विकसित
कृंतक हैं। ये
आस्ट्रेलिया के
अतिरिक्त अन्य सभी
महाद्वीपों में
पाई जाती हैं।
भारत की सबसे
साधारण पंचरेखिनी
गिलहरी (Funambulus
Pennanti) है, जिसके
गहरे भूरे शरीर
पर लंबाई की
दिशा में आगे
से पीछे तक जाती
है अपेक्षाकृत
हल्के रंग की पाँच
धारियाँ होती
है। यह मुख्य रूप
से उत्तरी भारत
में मनुष्य के निवासस्थानों
के आस-पास मिलती
हैं, इन्हें पाल भी
सकते हैं। दूसरी
साधारण गिलहरी
मुख्य रूप से दक्षिण
भारत में पाई
जानेवाली त्रिरेखिनी
है, जिसकी पीठ
पर केवल तीन
धारियाँ होती
हैं। ये जंगलों
में ही रहती हैं
और पकड़कर पालतू
बनाने का प्रयत्न
किए जाने पर कुछ
ही सप्ताहों में
मर जाती हैं।
गिलहरियों
की संबंधी आकंदलिकाएँ,
या उड़न गिलहरियाँ,
मुख्यत: वनचोरी
होती हैं। गरदन
के पीछे से लेकर
पिछली टाँगों
के अगले भाग तक
जाती हुई चर्मावतारिका
(Patagium) नामक
एक लोचदार झिल्ली
सरीखी रचना,
जो इनके सारे
धड़ से चिपकी रहती
है, इन प्राणियों
को ऊँचे-ऊँचे
पेड़ों से नीचे
भूमि पर, अथवा
निचली शाखाओं
पर, उतरने में
सहायता पहुँचाती
है। उड़न गिलहरियों
की इस गति को
हम उड़ान तो नहीं
कह सकते, विसर्पण
(gliding) अवश्य
कह सकते हैं। ये
प्राणी मुख्यत: एशिया
के उष्णप्रधान भागों
में पाए जाते हैं।
यद्यपि यूरोप
तथा उत्तरी अमरीका
में भी इनके प्रतिनिधियों
का अभाव नहीं है।
तीसरा
महत्वपूर्ण कुल
साइयूरिडी (Sciuridae)
हैं, जिसमें
वृक्षचारी गिलहरियाँ
(Ratufa),
उड़न गिलहरियाँ,
(Prtaurista) , स्थलचारी
गिलहरियाँ
(Citellus),
हिममूष (Marmoda),
चिपमंक (Tamias,
Eutamias) आदि
कृंतक आते हैं।
उपर्युक्त दोनों
कुलों के प्राणियों
से गिलहरियाँ
कुछ अधिक विकसित
कृंतक हैं। ये
आस्ट्रेलिया के
अतिरिक्त अन्य सभी
महाद्वीपों में
पाई जाती हैं।
भारत की सबसे
साधारण पंचरेखिनी
गिलहरी (Funambulus
Pennanti) है, जिसके
गहरे भूरे शरीर
पर लंबाई की
दिशा में आगे
से पीछे तक जाती
है अपेक्षाकृत
हल्के रंग की पाँच
धारियाँ होती
है। यह मुख्य रूप
से उत्तरी भारत
में मनुष्य के निवासस्थानों
के आस-पास मिलती
हैं, इन्हें पाल भी
सकते हैं। दूसरी
साधारण गिलहरी
मुख्य रूप से दक्षिण
भारत में पाई
जानेवाली त्रिरेखिनी
है, जिसकी पीठ
पर केवल तीन
धारियाँ होती
हैं। ये जंगलों
में ही रहती हैं
और पकड़कर पालतू
बनाने का प्रयत्न
किए जाने पर कुछ
ही सप्ताहों में
मर जाती हैं।
गिलहरियों
की संबंधी आकंदलिकाएँ,
या उड़न गिलहरियाँ,
मुख्यत: वनचोरी
होती हैं। गरदन
के पीछे से लेकर
पिछली टाँगों
के अगले भाग तक
जाती हुई चर्मावतारिका
(Patagium) नामक
एक लोचदार झिल्ली
सरीखी रचना,
जो इनके सारे
धड़ से चिपकी रहती
है, इन प्राणियों
को ऊँचे-ऊँचे
पेड़ों से नीचे
भूमि पर, अथवा
निचली शाखाओं
पर, उतरने में
सहायता पहुँचाती
है। उड़न गिलहरियों
की इस गति को
हम उड़ान तो नहीं
कह सकते, विसर्पण
(gliding) अवश्य
कह सकते हैं। ये
प्राणी मुख्यत: एशिया
के उष्णप्रधान भागों
में पाए जाते हैं।
यद्यपि यूरोप
तथा उत्तरी अमरीका
में भी इनके प्रतिनिधियों
का अभाव नहीं है।